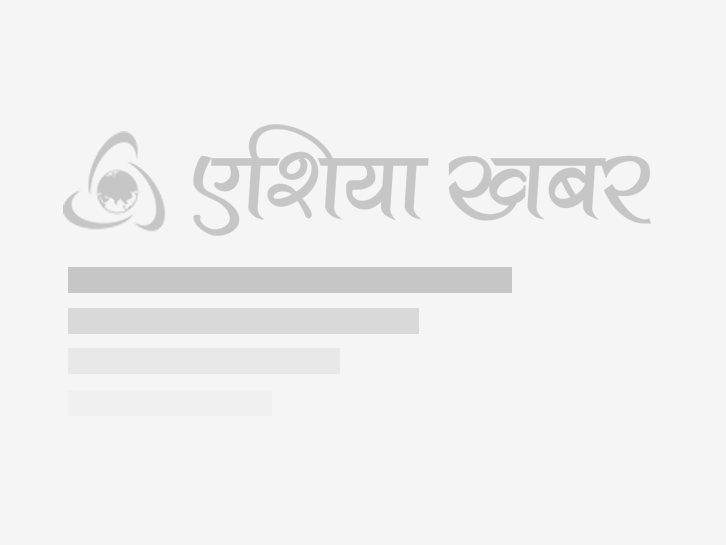
-सुनील कुमार महला-
वर्तमान में अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी से ठीक-ठाक गर्मी पड़ने लगी है। अभी से ही उत्तर भारत गर्मी का सामना करने लगा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हाल ही में इस संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का यह अनुमान है कि इस बार अप्रैल में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। गौरतलब है कि आईएमडी द्वारा कई इलाकों में ‘लू'(गर्म हवाएं)का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में 10 से 11 दिन लू चलने की संभावना है। कहना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने आने वाले महीनों में सामान्य से अधिक गर्मी और हीटवेव को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, वह जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट को इंगित करता है। आईएमडी के मुताबिक देश में अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत और उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में ‘लू’ चल सकती है। आशंका जताई गई है कि पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। वास्तव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप दिखेगा। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय वैश्विक तापमान(ग्लोबल वार्मिंग)में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे धरती पर गर्म लहरों की तीव्रता बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य, जीवों के स्वास्थ्य, वनस्पतियों और देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। सच तो यह है कि अत्यधिक गर्मी उधोगों और व्यवसायों के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करती है। कहना ग़लत नहीं होगा कि गर्मी बढ़ने से उत्पादकता में अभूतपूर्व कमी आती है। उच्च तापमान के संपर्क में आने वाले कर्मचारी गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे कार्य कुशलता कम हो जाती है और उत्पादकता प्रभावित होती है। अत्यधिक गर्मी आपूर्ति शृंखलाओं(जैसे कि परिवहन व रसद में देरी) को बाधित कर सकती है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, शीतलन उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की खपत में जबरदस्त वृद्धि होती है। यह बढ़ी हुई मांग बिजली ग्रिड पर दबाव डालती है, जिससे संभावित रूप से बिजली की कटौती होती है और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर व्यवसायों पर असर पड़ता है और ऊर्जा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। कहना चाहूंगा कि अत्यधिक गर्मी से कई तरह से वित्तीय नुकसान हो सकता है, जिसमें कृषि में फसल की विफलता, पर्यटन पर निर्भर व्यवसायों के लिए पैदल यातायात में कमी, तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के रख-रखाव की लागत में वृद्धि शामिल है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि मौसम वैज्ञानिक बहुत लंबे समय से यह चेतावनी जारी कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग(वैश्विक तापमान) में बढ़ोत्तरी की वजह से दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। गौरतलब है कि पिछले ही वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में पहली हीटवेव ओडिशा में अप्रैल की शुरुआत में महसूस की गई थी, जबकि इस वर्ष कोंकण व तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फरवरी का अंत आते-आते ही होटवेव जैसी स्थितियां पैदा होने से मौसम को लेकर पहले ही अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। यह बात ठीक है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को एकदम से रातों-रात नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम गर्मी रोकने वाली गैसों और कालाशे कार्बन के मानव उत्सर्जन को कम करके इसकी दर को धीमा कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा को काफी हद तक सीमित कर सकते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्याओं को समायोजित करके भी हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मसलन, रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण), परिवहन के तरीकों को बदलकर, भोजन की बर्बादी को रोककर, अपनी ऊर्जा खपत का उचित प्रबंधन करके तथा दूसरों को पर्यावरण के प्रति शिक्षित और जागरूक करके काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। आज विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि हो रही है और इसके लिए मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना जिम्मेदार ठहराते जा सकते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि ये गतिविधियाँ ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ती हैं, और हमारे नीले ग्रह के नाजुक जलवायु संतुलन को बिगाड़ती हैं। संक्षेप में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि से है और यही तापमान वैश्विक जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। सच तो यह है कि तापमान में निरंतर वृद्धि दुनिया भर में व्यवधानों को बढ़ावा देती है। मसलन, अधिक चरम गर्मी पिघलती बर्फ की टोपियों से लेकर बारिश के बदलते पैटर्न तक, कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ता है। ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलने लगतीं हैं। उच्च तापमान से तूफान, वन्य आग, बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैव-विविधता की हानि होती है। सच तो यह है कि आज कई प्रजातियां बदलती जलवायु के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप विलुप्ति हो रही है। तापमान बढ़ोत्तरी से महासागरों का अम्लीकरण होता है। इससे अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों में घुल जाती है, जिससे पीएच स्तर में परिवर्तन होता है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। धरती का तापमान बढ़ता है तो भोजन एवं पानी की कमी हो जाती है। सच तो यह है कि सूखे और अनियमित मौसम से फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। वायु प्रदूषण और अत्यधिक गर्मी श्वसन संबंधी बीमारियों और हीटस्ट्रोक में योगदान देती है। संक्षेप में कहें तो इससे स्वास्थ्य पर संकट बढ़ते हैं। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि यदि हमने समय रहते अपने कार्बन उत्सर्जन(ग्रीन हाउस गैसों) को नियंत्रित नहीं किया और पर्यावरण संरक्षण को उचित प्राथमिकता नहीं दी, तो आने वाले वर्षों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। आज वनों की कटाई, चरागाहों में लगातार कमी और अनियंत्रित औधोगिकीकरण और शहरीकरण ने मौसम चक्र को असंतुलित किया है, जिससे मौसम संबंधी असामान्य घटनाएं भारत समेत पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। पाठकों को बताता चलूं कि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो वर्ष 2015 में पेरिस में हुआ था लेकिन अमेरिका ने पेरिस समझौते से दूरी बनाकर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। पाठकों को बताता चलूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह समझौता अमेरिकी आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका तो अमेरिका ग्रीनहाउस गैसों(कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि) के उत्सर्जन के लिए चीन, भारत, रूस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जापान, ईरान, और कनाडा जैसे देश ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। एक जानकारी के अनुसार इन देशों ने साल 2020 में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का करीब 67% हिस्सा अदा किया था। एक अन्य उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, रूस और ब्राजील वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे बड़े जीएचजी(ग्रीन हाउस गैस) उत्सर्जक थे। साथ में वे वैश्विक जनसंख्या का 49.8%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 63.2%, वैश्विक जीवाश्म ईंधन खपत का 64.2% और वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन का 62.7% हिस्सा हैं। इन शीर्ष उत्सर्जकों में से, वर्ष 2023 में चीन, भारत, रूस और ब्राजील ने वर्ष 2022 की तुलना में अपने उत्सर्जन में वृद्धि की, जिसमें भारत में सापेक्ष रूप से सबसे बड़ी वृद्धि (+ 6.1%) और चीन में 784 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी निरपेक्ष वृद्धि हुई। यह विडंबना ही है कि आज विकसित देश विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन खुद इन गैसों पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सौर व ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर जोर दें, ताकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। पाठकों को बताता चलूं कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में सौर ऊर्जा के अलावा क्रमशः पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, इथेनॉल, तरंग और ज्वारीय ऊर्जा को शामिल किया जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक और स्व-पुनःपूर्ति करने वाली ऊर्जा होती है तथा इनका कार्बन फ़ुटप्रिंट कम या शून्य होता है। इतना ही नहीं, ये ऊर्जा स्रोत कभी खत्म भी नहीं होते हैं। वास्तव में, इनका इस्तेमाल करके हम जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं, क्यों कि इनमें से कई संसाधन सीधे वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। जल और ऊर्जा की बचत करनी होगी अथवा इनका मितव्ययिता के साथ विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से तभी बचा जा सकता है जब हम जागरूक होकर जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए आगे आए, प्रकृति व इसके संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न करें।
