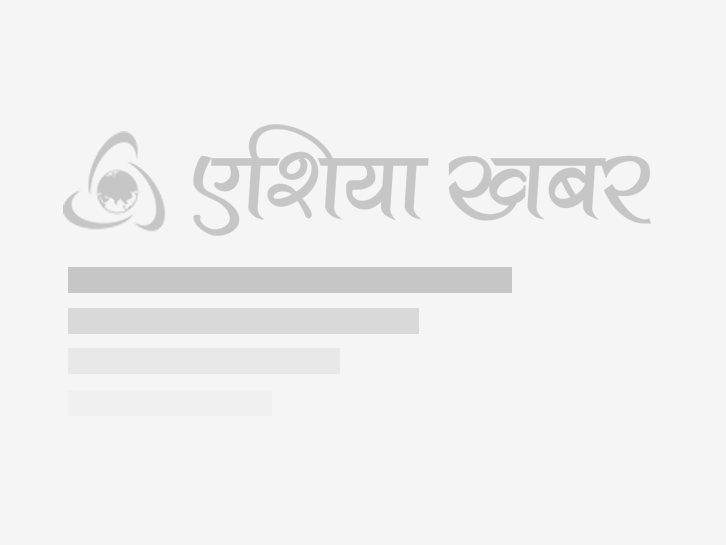
गर सरलीकरण करना हो तो कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भगवा रंग खिलने का फौरन असर हिन्दी पट्टी की सियासत पर दिखा। कोई यह दलील दे सकता है कि नगालैंड और मेघालय में तो स्थानीय सियासी समीकरणों और केंद्र में सत्ता और प्रचुर संसाधनों का लाभ भाजपा को मिला लेकिन त्रिपुरा के मामले में शायद यह एक हद तक ही सही है। त्रिपुरा में वाम मोर्चा और कांग्रेस का ही अस्तित्व था, जो देश की मुख्यधारा की पार्टियां हैं। यानी मुख्यधारा के वामपक्षीय मध्यमार्गी पार्टियों का स्थान तेजी से भाजपा लेती जा रही है। शायद यह एहसास ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ बहुजन समाज पार्टी की मायावती को दो संसदीय उपचुनाव गोरखपुर और फूलपूर में एक मंच पर लाने की फौरी वजह बना। वरना मायावती अभी भी तय नहीं कर पा रही थीं कि सपा के साथ एक पाले में बैठने का क्या औचित्य है? हालांकि मायावती ने फौरन यह भी साफ कर दिया कि सपा उम्मीदवारों को यह समर्थन तात्कालिक है और इसका अर्थ यह न लगाया जाए कि यह 2019 के आम चुनाव की पूर्व पीठिका है। लेकिन गोरखपुर और इलाहाबाद में बसपा के पार्टी प्रभारियों के बयानों पर गौर करें तो लगता है कि बसपा में भी यह एहसास गहरा रहा है कि इसके बिना कोई चारा नहीं है। यह एहसास बसपा या मायावती को ही नहीं, सभी गैर-भाजपा दलों में जल्दीबाजी का भाव पैदा करता लगता है। मायावती के ऐलान के बाद फौरन अजित सिंह की अगुआई वाले राष्ट्रीय लोकदल ने भी दोनों उपचुनावों में सपा उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान कर दिया है। रालोद का पूर्वी उत्तर प्रदेश में समर्थन सांकेतिक महत्त्व का ही है, मगर इससे सियासी हवा का अंदाजा लगता है। कांग्रेस के उम्मीदवार जरूर दोनोें सीटों पर खड़े हैं लेकिन नये समीकरणों में उसकी रणनीति क्या होगी, यह देखना होगा।गोरखपुर और फूलपुर दोनों संसदीय सीटें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उप मुख्यमंत्री केशवचंद्र मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई हैं। इसलिए भाजपा के लिए यह नाक का सवाल भी है। इसी वजह से भाजपा में थोड़ी बेचैनी दिख सकती है। लेकिन अगले साल फिर चुनाव होने हैं। इसलिए ये चुनाव 2019 की तैयारी का हिस्सा ही कहला सकते हैं। वैसे आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा के लिए भी ज्यादा ढीलापन दिखाने की गुंजाइश नहीं है। 2014 के लोक सभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर भाजपा को करीब 51 प्रतिात वोट मिले थे, जबकि सपा को करीब 23 प्रतिशत और बसपा को करीब 17.5 प्रतिशत वोट मिले थे। यानी दोनों के वोटों में कांग्रेस के करीब आठ प्रतिात वोट को भी जोड़ लें तब भी भाजपा ऊपर ही बैठती है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव का गणित अलग है। दोनों ही सीटों पर पांच विधान सभाओं में से चार सपा या बसपा को बढ़त वाली हैं। यही गणित सपा-बसपा को मिलकर भाजपा को चुनौती देने की उम्मीद जगा रहा है। हालांकि आदित्यनाथ सरकार से लोगों के मोहभंग का अभी वैसा कोई बड़ा संकेत नहीं हैं। केंद्र की सरकार के प्रति नाराजगी तो कई वजहों से दिख सकती है। क्योंकि किसी योजना का खास असर होता नहीं दिख रहा है और लोग महंगाई, रोजगार की कमी, अर्थव्यवस्था में मंदी वगैरह से परेशान हैं। इसका असर हाल में राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में दिखा भी। इसलिए कुछ लोगों का अनुमान है कि पूर्वोत्तर के नतीजे भले माहौल बनाएं और भाजपा में नया उत्साह भर दें लेकिन भाजपा को अपने शासन वाले राज्यों में लोगों की नाराजगी से दो-चार होना पड़ेगा। जैसा कि हाल के गुजरात विधानसभा चुनाव में दिखा भी। वहां भाजपा किसी तरह जीत तो गई लेकिन जश्न मनाने का मौका कांग्रेस के हाथ लगा था। यह समझ भी मायावती को बाकी दलों से गठजोड़ कायम करने की ओर ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी राज्यों में भी भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के दो उपचुनाव में इस गणित पर भी र्चचा हुई कि अगर वहां बसपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए होते तो कांग्रेस की जीत का अंतर इतना कम नहीं होता। यानी बसपा के न होने से उसके वोट भाजपा की ओर चले गए। तो, ऐसे गणित लगाए जाने लगे हैं।मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में मायावती के घाव कुरेदने के लिए लखनऊ के उस गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, जो सपा-बसपा के बीच गहरी खाई की तरह बना हुआ है। हालांकि यह भी सही है कि तब से गोमती में काफी पानी बह चुका है। सपा का नेतृत्व भी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के हाथ से फिसलकर आखिलेश यादव के हाथ आ गया है। अखिलेश अपनी ओर से कोई तीखा बयान नहीं देते और हमेशा मायावती को बुआ कहकर संबोधित करते हैं। मायावती के तेवर भी अखिलेश के लिए उतने तल्ख नहीं हैं। लेकिन इस व्यक्तिगत पसंदगी-नापसंदगी से ज्यादा बड़ा वह सामाजिक समीकरण है, जो सपा-बसपा की विभाजक रेखा रहा है। सपा का वोटबैंक मुख्यत: यादव और मुसलमान हैं जबकि बसपा का मुख्य आधार जाटव हैं। यादवों और जाटवों के बीच सामाजिक तनाव ऊंची जातियों के मुकाबले भी ज्यादा ही माना जाता है। इसलिए दोनों को एक पाले में खड़ा करना आसान नहीं है। हालांकि इधर योगी सरकार की एनकाउंटर मुहिम के निशाने पर कथित तौर पर सपा और बसपा समर्थक बताए जाते हैं। इससे भी एक एका का भाव पैदा हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि अब 21 राज्यों में परचम लहरा चुकी भाजपा देश में मुख्य दल का स्थान ग्रहण करती जा रही है और अब वह सिर्फ ब्राrाण, बनिया पार्टी नहीं रही। उसे किसी भी तरह अपने को लचीला बनाने से गुरेज नहीं है, जैसा कि पूर्वोत्तर में उसने ईसाई समूहों की संवेदना को देखते हुए बीफ पर लचीला रुख अपना लिया। इसलिए दूसरे मध्यमार्गी दल एक होकर ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। यह देखना है कि सपा-बसपा की यह यारी कितने समय तक रहती है। फिलहाल तो सुविधा यह है कि बसपा उपचुनाव लड़ने में यकीन नहीं करती इसलिए समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम चुनाव में हर क्षेत्र में हित टकराएंगे तो क्या गणित उभरता है, यह देखना होगा। फिर, अगर इस एका के बावजूद गोरखपुर और फूलपुर सपा हार जाती है, तब भी नये सिरे से गणित पर विचार हो सकता है।
