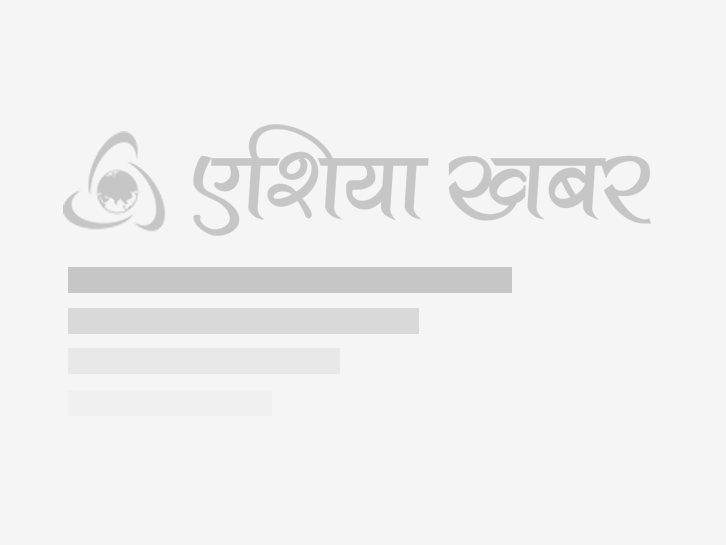
-गिरीश्वर मिश्र-
अक्सर भाषा को संचार और अभिव्यक्ति के एक प्रतीकात्मक माध्यम के रूप ग्रहण किया जाता है। यह स्वाभाविक
भी है। हम अपने विचार, सुख-दुख के भाव और दृष्टिकोण दूसरों तक मुख्यत: भाषा द्वारा ही पहुंचाते हैं और संवाद
संभव होता है।
निश्चय ही यह भाषा की बड़ी भूमिका है परंतु इससे भाषा की शक्ति का केवल आंशिक परिचय ही मिलता है
क्योंकि शायद ही कुछ ऐसा अस्तित्व में हो जो भाषा से अनुप्राणित न हो। भाषा से जुड़ कर ही वस्तुओं की अर्थवत्ता
का ग्रहण हो पाता है। यही सोच कर भाषा को जगत की सत्ता और उसके अनुभव की सीमा भी कहा जाता है।
सचमुच जो कुछ अस्तित्व में है वह समग्रता में भाषा से अनुविद्ध है।
सत्य तो यही है कि भाषा मनुष्य जाति की ऐसी रचना है जो स्वयं मनुष्य को रचती चलती है और अपनी
सृजनात्मक शक्ति से नित्य नई नई संभावनाओं के द्वार खोलती चलती है। हम ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और
कला आदि अर्थात सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत शामिल उन सभी तत्वों का अनुभव जिन पर हम गर्व करते हैं,
भाषा के द्वारा ही कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में भाषाई निपुणता मनुष्यता का पर्याय हो जाती है। ऐसे में भाषा
अतुलनीय संपदा का रूप ले लेती है और तब यह सापेक्षिक वर्चस्व से जुड़ जाती है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा से
संबद्ध होकर स्वयं भाषा का अस्तित्व राज-सत्ता पर आश्रित होने लगता है। सत्ता के समीकरण के साथ भाषाओं का
दायरा संकुचित या विस्तृत होता रहता है।
यह एक सुखद आश्चर्य है कि भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का एक अत्यंत समृद्ध देश है जहां सहस्राब्दियों से
कई भाषाओं का प्रयोग होता आया है। इस क्रम में अवाचिक चरण से होकर लिपि के आविष्कार और उपयोग के
साथ कई भाषाओं के प्रचुर साहित्य की उपस्थिति दर्ज हुई है। सिर्फ संस्कृत भाषा को ही लें, जो एक अतिप्राचीन
भाषा है, तो भारत की विकसित ज्ञान-परम्परा की विशदता और गहनता का पता सहज में लग सकता है और यह
भी मालूम हो सकता है कि इस महान भाषा को किस षड्यंत्र से ज्ञान की औपचारिक या प्रामाणिक व्यवस्था से ही
बहिष्कृत कर दिया गया।
चूंकि भाषा में ही संस्कृति बसती है इसलिए संस्कृत को परे ढकेल कर भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की
अंग्रेजों की योजना कामयाब हो गई। तब अपनी ही संस्कृति पराई लगने लगी और उसके जीवन-मूल्य संदेह के घेरे
में आ गए। दूसरी ओर अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने भारतीय उपनिवेश में अपनी प्रभु-सत्ता की विशिष्टता स्थापित
करने के लिए अंग्रेजी भाषा को जिस तरह से भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में स्थापित किया। इसके द्वारा अंग्रेजों ने
सोच-विचार और व्यवहार को इस तरह अंग्रेजीमय बना दिया कि अंग्रेजी ही प्रामाणिक हो गई और शिक्षा, स्वास्थ्य,
कानून अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उसका दबदबा स्थापित होता गया। दूसरी ओर भारतीय भाषाओं के साथ एक
किस्म की हीनता की भावना जुड़ गई। चूंकि भाषा का आत्म-गौरव और अस्मिता के साथ गहरा संबंध होता है
इसलिए इसका व्यापक असर देश के साथ जुड़ाव पर भी पड़ता रहा।
अंग्रेजी भाषा के अभूतपूर्व प्रभुत्व ने भारतीय मानस में एक मूल्य और आदर्श का स्थान ले लिया। हमने यह नहीं
देखा कि जर्मन, फ्रांसीसी, स्पैनी, चीनी, रूसी, जापानी, कोरियाई और हिब्रू आदि भाषाओं में पढ़-लिखकर भी
अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करने की क्षमता विकसित होती है। इन सब देशों में विश्व
स्तर के विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं। हम लोगों के नेताओं के मन में यह भाव घर कर गया कि अंग्रेजी ही
दुनिया के लिए, ज्ञान और प्रगति के लिए इकलौती राह है। हमने अंग्रेजी वाली विचार-दृष्टि को एक सार्वभौमिक
सत्य मान लिया और उसी का गुणानुवाद करने में जुटे रहे। इस दुराग्रह के प्रभाव में अंग्रेजी भाषा भारतीय समाज
को जड़ों से काटने, उसे मौलिक चिंतन से महरूम करने और पर निर्भर बने रहने के लिए अभिशप्त करती रही. हम
निरुपाय हो गए और अंग्रेजी की जकड़ इतनी मजबूत होती गई कि स्वतंत्र होने के सत्तर साल बीतने के बाद भी
आज देश में भाषाई और स्वराज का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। फलत: मन और बुद्धि बंधक हो चली है और
विचारों में भी स्वराज नहीं आ सका।
यह ध्यातव्य है कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी हम वहां नहीं पहुंच सके जो अभीष्ट था और जहां पहुंचना चाहिए
था। आज भी कोई विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा का संस्थान विकसित नहीं हो सका है और हमारी ज्ञान-दृष्टि
अधिकांशत: यूरोप और अमेरिका की छाया मात्र ही बन सकी। हमारे मेधावी छात्र अध्यापक उन्हीं को संदर्भ बिंदु
मानते हैं। इस पृष्ठभूमि में हम भारत को भारत की दृष्टि से देखने का कोई अभ्यास ही विकसित नहीं कर सके
और उसकी उपादेयता के बारे में भी संशय बना रहा। अब जब वैश्वीकरण का दौर चला तो फिर ज्ञान और ज्ञान की
पद्धति का पश्चिम से आयात कुछ और तीव्र हो गया। हम विशेषज्ञता के लिए पश्चिम की ओर मुंह किए रहते हैं।
पूर्व और पश्चिम के बीच ज्ञान-विज्ञान का विनिमय पर यह सारा उपक्रम एकतरफा होकर रह गया। अल्पकालिक
दृष्टि से इस युक्ति के कुछ लाभ हो सकते हैं परंतु दूरगामी दृष्टि से इसके नुकसान ही हैं।
सामाजिक दृष्टि से देखें तो भाषा के उपयोग को लेकर भारत एक बहुभाषी समाज के रूप में उपस्थित होता है और
अनेक भारतीय भाषाएं साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध हैं। सामान्य जीवन के अनौपचरिक क्षेत्रों (यथा-बाजार,
मनोरंजन, घर परिवार) में भाषाई विविधता दिखती है। जनसंचार माध्यमों में भी इसका संज्ञान लिया जा रहा है
परंतु ज्ञान निर्माण और प्रशासन में अंग्रेजी ही हावी है।
देश में भाषा को लेकर संजीदगी से विचार नहीं हो पा रहा है। अभी तक कोई भाषाई नीति नहीं बन सकी है और
इसके कई दुष्परिणाम हो रहे हैं। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के बाहुल्य और प्राबल्य के चलते, जो केवल दस-बारह
प्रतिशत भारतीयों की समझ में आती है, अधिकांश जन-जीवन में क्षोभ और कठिनाई का अनुभव होता है। इससे
अनपेक्षित रूप से कार्य-हानि, विभिन्न अवसरों पर भेद-भाव और गैर-अंग्रेजीदां भारतीयों की मानवीय गरिमा को
हानि पहुंचती है। फलत: मानवाधिकार के हनन की सी स्थिति बनती है।
शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग सर्वत्र स्वीकृत है तथापि अंग्रेजी को थोपने का प्रयास चालू है।
यह बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों के लिए हानिकारक है। इस तथ्य की सतत अनदेखी की जाती रही है और
अभी भी कोई स्पष्ट नीति उपयोग में नहीं आ रही है। विद्यालयों में भाषा-अध्ययन के स्वरूप को त्रिभाषा सूत्र के
अंतर्गत व्यवस्थित किया गया ताकि पूरे देश में विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार हो। परंतु यह कार्य अभी तक
समुचित रूप से नहीं हो सका है।
भारतीय संविधान ने निर्विवाद रूप से हिंदी को राज भाषा के रूप में स्वीकार किया और अंग्रेजी के उपयोग को तब
तक सशर्त अनुमति दी जब तक हिंदी के प्रयोग की तैयारी पूरी न हो जाय। यह विचार समस्त देश के लिए एक
संपर्क भाषा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया। व्यावहारिक स्तर पर इस कार्य के लिए कई उपाय भी
शुरू हुए। राज-भाषा विभाग की स्थापना के साथ ही, शब्दकोश तथा पुस्तक आदि सामग्री का निर्माण, भाषा
तकनीकी का विकास, भाषा-प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन आदि के प्रयास होते रहे परंतु राजनीतिक दांवपेंच और सरकारी
कार्य शैली की शिथिलता के फलस्वरूप हिंदी की उपयुक्त्तता / पात्रता की तिथि निरंतर टलती ही गई और अब वह
राजनेताओं की मर्जी पर टिकी हुई है। उपेक्षा के कारण भाषा के प्रति दृष्टिकोण में गंभीरता नहीं आ सकी और हिंदी
को लेकर दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा / मास की उत्सवधर्मिता से आगे बढ़कर स्थायी कार्य नहीं हो सका। ऐसे ही
विभिन्न सरकारी संस्थान पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सके हैं।
उल्लेखनीय है कि किसी भी देश की उपलब्धि केवल आर्थिक पैमानों पर नहीं आंकी जा सकती। यह दुर्भाग्य ही कहा
जाएगा कि भाषा के रूप में प्राप्त विरासत को संभालने और उसे संबर्धित करते हुए स्वयं को सम्पन्न बनाने की
ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा सका। इसका परिणाम नई पीढ़ी में भाषा और
संस्कृति के संस्कारों के दुर्बल होने में दिख रही है। यह स्थिति सुधी जनों तथा समाज के हितैषियों के लिए समान
रूप से चिंतनीय है। इस तरह के सरोकारों पर चिंतन और उपयोगी हस्तक्षेप के लिए गैर सरकारी संगठनों की विशेष
भूमिका है। आज आवश्यक है कि लोकभाषा हिंदी ज्ञान की भाषा बने और हम उसके उपयोग में गौरव का बोध करें।
राजभाषा की प्रतीकात्मक सत्ता को जन व्यवहार में स्थापित करना ही एकमात्र विकल्प है।
