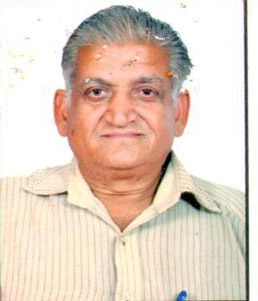
सुरेंदर कुमार चोपड़ा
अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा हुआ
है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक
शक्तियों को केंद्रीय व प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। नतीजतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील
रहती है, जो देश की अखंडता व संप्रभुता के प्रति जवाबदेह होती है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है।
गोया, यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बंटता है और समय व पूंजी का क्षरण होता
है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है,
फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। इन सब मुद्दों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के आरंभ से ही एक देश, एक चुनाव की पैरवी कर रहे हैं, तो इसे विपक्षी दलों को
गंभीरता से लेने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मुद्दे को रेखांकित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने
एकबार फिर इस मुद्दे को संविधान दिवस पर उठाकर जता दिया है कि वे इसपर गंभीर हैं और इसका हल जरूर
निकालेंगे।
हालांकि एकसाथ चुनाव आसान नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री यदि निर्विवाद सोच के साथ इस दिशा में कोई पहल कर
रहे हैं तो सम्पूर्ण विपक्ष को इसे जल्द हल करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। विधि आयोग ही नहीं निर्वाचन
आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक
संस्थाएं हैं। वैसे भी यदि एकसाथ चुनाव होते हैं तो सरकार को नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिए
अधिक समय मिलेगा। फिलहाल चुनाव की घोषणा होते ही, आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। नतीजतन
केंद्र व राज्य सरकारें पंगु हो जाती हैं। स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों को भी हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना
पड़ता है। इसलिए मांग तो यह भी हो रही है कि लोक व विधानसभा के साथ निकायों व पंचायत के भी चुनाव
कराए जाएं।
एकसाथ चुनाव के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मोड पर आ जाता है, लिहाजा
सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती ही हैं, नीतियों को कानूनी रूप में देने में अतिरिक्त विलंब भी
होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है। इसलिए सभी राजनितिक दलों को आत्म-मंथन की जरूरत है, क्योंकि
इस मुद्दे में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केवल सत्तारूढ़ दल को ही फायदा हो? इसलिए अब प्रत्येक दल को आगे
आकर प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि यह कैसे संभव होगा और इसे अमल में लाने का तरीका क्या होगा? वैसे भी
राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है जब वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी भागीदारी करें। नीतिगत फैैसलों को अधिकतम
लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुझाव दें व उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं।
ऐसा नहीं है कि एकसाथ चुनाव का विचार नरेंद्र मोदी का कोई सर्वथा मौलिक विचार है। 1952 से लेकर 1967
तक चार बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए हैं। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर
वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेष व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो
गया। इंदिरा गांधी को विपक्ष की जो सरकार पसंद नहीं आती थी, उसे वे कोई न कोई बहाना ढूंढकर बर्खास्त कर
देती थीं। नतीजतन मध्यावधि चुनावों की परिपाटी पड़ती चली गई। इससे राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव
कराने की बाध्यता निर्मित हो गई। फलतः ऐसा अवसर आ गया कि देश में कहीं न कहीं चुनाव की डुगडुगी बजती
रहती है। देश का लगभग 88 करोड़ मतदाता किसी न किसी चुनाव की उलझन में जकड़ा रहता है। संविधान में
लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एकसाथ कराने का हवाला नहीं है।
संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है, लेकिन
बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिर या गिराई जा
सकती है। लिहाजा एकसाथ चुनाव कराने की संभावना तब बनेगी, जब संविधान में संशोधन किए जाएं, जिनका
किया जाना कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है।
चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर
किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए।
लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो
जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एकसाथ चुनाव के लिए कम से कम पांच अनुच्छेदों
में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। यह एक कठिन प्रक्रिया है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को
प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो 'रचनात्मक अविश्वास' मत
हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते
हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर
नई सरकार शपथ दिला दी जाए।' इसी के साथ दूसरा प्रस्ताव यह भी था कि 'लोकसभा चुनाव के साथ
विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए उनकी अवधि एक मर्तबा कम कर दी जाए, लेकिन इस प्रस्ताव पर अमल
के लिए भी संविधान में संशोधन जरूरी है।'
कुछ विपक्षी दल एकसाथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस
दल ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्य सरकारें उसी दल की होंगी? जैसे कि सत्रहवीं
लोकसभा के चुनाव में देखने में आया था। इस चुनाव में राष्ट्रवाद की हवा के चलते राजग को बड़ा जनादेश मिला।
ऐसे में यदि विधानसभाओं के भी चुनाव हुए होते तो कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों का भी सूपड़ा साफ हो गया जायेगा?
हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसबार लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा, आंध्र-प्रदेश, सिक्किम, तेलांगाना और अरुणाचल
प्रदेश में भी चुनाव हुए, इनमें परिणामों में भिन्नता देखने में आई। लिहाजा यह दलील बेबुनियाद है कि एकसाथ
चुनाव में क्षेत्रीय दल नुकसान में रहेंगे।
बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को यह भय भी बना रहता है कि
उसका कोई नीतिगत फैसला ऐसा न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं। लिहाजा सरकारों को
लोक-लुभावन फैसले लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका सहित अनेक ऐसे देश हैं, जहां एकसाथ चुनाव बिना किसी
बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एकसाथ चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो केंद्र व राज्य
सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोकहित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास व सुशासन
को सुचारू रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा। इसलिए विपक्षी दलों को राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते
हुए इस पहल को समर्थन देने की जरूरत है।
