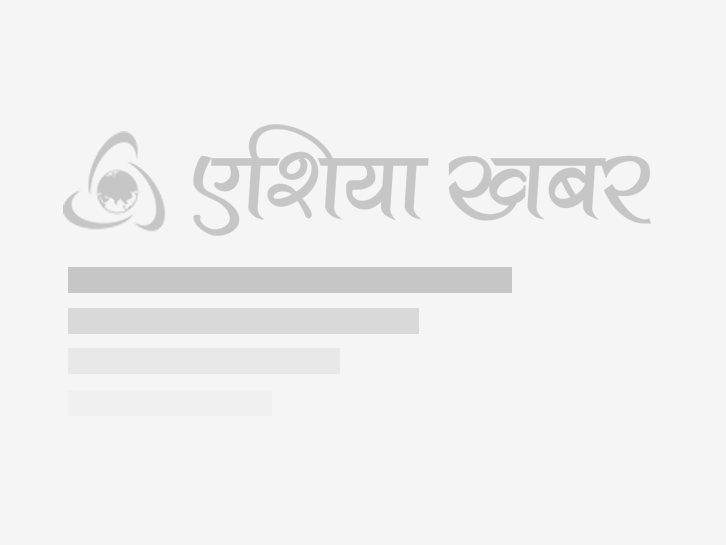
साल नई इबारतें लेकर आया है। 21वीं सदी की पहली पीढ़ी बालिग हो रही है, और क्षितिज पर संभावनाओं और चुनौतियों के बादल घुमड़ रहे हैं। नई वयस्क पीढ़ी को शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा, रोजगार और कॅरियर चयन की उलझनों से तो मुकाबिल होना ही है, बेहद उलझे राजनैतिक विकल्पों का चयन भी उसकी बाट जोह रहा है। आखिर, उसके वोट देने की उम्र हासिल करने का साल 2018 ऐसा विरला होगा जब शुरुआत से अंत तक चुनावों की गहमागहमी ही जारी रहेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते वर्ष 2017 के आखिरी दिन अपने वष्ात में मन की बात में उनसे वोट की बात की और उम्मीद जताई कि वह राजनीति को नई दिशा देगी। अभी दहलीज पर पांव रख रही पीढ़ी से यह उम्मीद कुछ नाइंसाफी-सी लगती है। लेकिन कोई करे भी क्या? इस साल चुनावी राजनीति किसी और चीज के लिए फुर्सत देती नहीं लगती है, खासकर ऐसे माहौल में जब दांव सबसे ऊंचे लगे हों। आखिर, आठ राज्यों-मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक (साल के शुरू में) और मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान (साल की आखिरी तिमाही में)-के चुनाव होते ही अगले साल यानी 2019 में आम चुनावों की वेला आ जाएगी। फिर बीता वर्ष जाते-जाते राजनीति, अर्थव्यवस्था यानी सभी को ऐसा गड्डमड्ड कर गया है कि संभावनाओं और आशंकाओं के बीच बेहद महीन फर्क ही रह गया है।राजनीतिक मोर्चे पर गुजरात चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुआई में भाजपा जीत तो गई लेकिन खुशी खिली विपक्ष में। विपक्ष खासकर कांग्रेस में तो हारकर भी ऐसा उत्साह लौट आया कि उसमें आक्रामकता लौट आई है। दरअसल, कांग्रेस से भी बढ़कर गुजरात में युवा नेताओं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी ने भाजपा और मोदी की अपराजेय-सी छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए और उनके विकास के गुजरात मॉडल को संदिग्ध बना दिया। फिर, नोटबंदी और जीएसटी के नतीजों ने भी सरकार हाथ खाली कर दिए। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े 6.5 फीसदी आए और सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि जीएसटी नोटबंदी से प्रभावित नहीं हुई लेकिन भाजपा के ही राज्य सभा सदस्य सुब्रrाण्यम स्वामी ने यह खुलासा करके उसे बेमजा कर दिया कि ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पर दबाव डालकर हासिल किए गए हैं। इसी तरह अभी जीएसटी की पेचीदगी की वजह से राजस्व उगाही में भारी कमी के आंकड़े भी आ गए हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका है यानी सरकार चाह कर भी इस साल अपने आखिरी पूर्ण बजट में बहुत कुछ लुभावने प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। एक अटकल यह भी लगाई जा रही है कि सरकार इस कमी की भरपाई के लिए विश्व बैंक से 50 अरब डॉलर का कर्ज लेने की सोच रही है। जाहिर है, लगभग दो-ढाई दशक बाद देश के सामने ऐसे हालात मौजूद होंगे। मामला सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था का ही नहीं है, समाज भी कई तरह के सवालों से रू-ब-रू है। युवा, महिला, किसान, छोटे व्यापारी हर ओर एक बेचैनी-सी दिखाई पड़ रही है। इसे चुनावी जीत-हार से अब शायद ही ढंका जा सके। बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि रोजगारविहिन आर्थिक वृद्धि के आंकड़े अब लुभाते नहीं हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग में सुधार आास्ति जगाने के बदले गहरे सवाल पैदा कर रही है। सुब्रrाण्यम स्वामी ने ही कहा है कि ये आंकड़े तो पैसे देकर हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर समाज में हो रही हलचलें हैं। गुजरात में सबसे तीखा विभाजन, चुनावी नतीजों के संदर्भ में, गांव और शहर के बीच दिखा। इससे विकास के र्ढे पर गहरे सवाल खड़े हुए हैं। गुजरात ही क्यों, पूरे देश में दलित और पिछड़ी जातियां ही नहीं, अब तक ताकतवर और संपन्न मानी जाने वाली जातियां भी संकट महसूस कर रही हैं। अलग-अलग हिस्सों में जाट, कापू, मराठा, गुर्जर अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, सवर्ण जातियों की ओर से भी आरक्षण की मांग उठ रही है। यह उस संकट की ओर इशारा है, जो नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों से निकले विकास के तौर-तरीकों से पैदा हुए हैं। किसान, मजदूर, समाज के पुराने ताकतवर तबके, छोटे व्यापारी सब खस्ताहाल हैं। मगर बड़े उद्योगपतियों की संपत्तियों में लगातार इजाफा हो रहा है। बेशक, इस सदी के शुरू में मध्य वर्ग को कुछ नौकरियां मिलीं। नये हुनर के लिए शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण भी हुआ और देश में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ आ गई लेकिन अब सुनहरा सपना टूट रहा है। नौकरियां भी सिमटीं और थोक भाव में ऐसे निजी संस्थानों के बंद होने की खबरें भी आने लगीं। ऐसे माहौल में 18 वर्ष में प्रवेश कर बालिग हो रही 21वीं सदी की पहली पीढ़ी के सामने हकीकत की नई परतें खुलती दिख रही हैं। पिछली सदी के आखिरी दशक में पैदा हुई पीढ़ी भी ऐसी ही हकीकत से 2010-11 में हुई थी, जिसके नजारे अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान दिखे थे। उससे राजनीति की फिजा एकबारगी बदल गई थी। मगर उससे विकास की धारा नहीं बदली, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण के जरिए एक नई फिजा तैयार हुई, जिसमें अन्ना आंदोलन के दौरान समाज को पारदर्शी बनाने के मुद्दे ही नेपय में चले गए। अब लोकपाल, याराना पूंजीवाद जैसे मुद्दों पर अब बात भी नहीं होती लेकिन उसके दंश डूबत कर्ज से लेकर कई मामलों में दिखते हैं। याद करें 21वीं सदी को भारत की तस्वीर बदलने के सपने के रूप में पेश किया जाता रहा है। लेकिन यह सदी तो और चुनौतियां लेकर आ रही है। लेकिन ऐसे ही चुनौतीपूर्ण महौल में उम्मीद की कोपलें भी फूटती हैं। दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास भी कोई वैकल्पिक नजरिया नहीं है। इसलिए यह कहने में कोई अति-उक्ति जैसी बात नहीं होगी कि नई पीढ़ी को अपने सभी विकल्पों पर खूब सोचना-विचारना पड़ सकता है।
