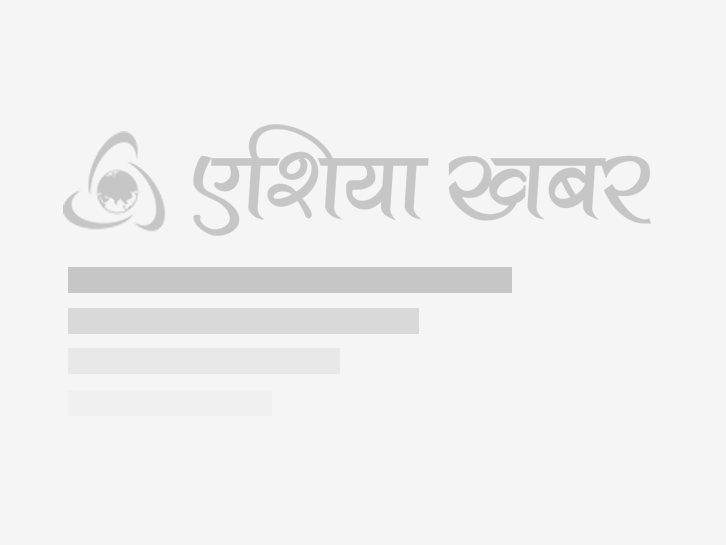
अनेक ‘शुभचिंतक’ राजनीतिक दलों के चलते भी जातीय भेदभावों के ख़िलाफ़ दलितों की लड़ाई और लम्बी होती जा रही
है। ये ‘शुभचिंतक’ राजनीतिक दल दलितों के वोट तो पाना चाहते हैं लेकिन उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई
कार्यवाही न करके कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। कारण है कि यदि वो अत्याचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही
करेंगे तो अत्यचारियों का वोट उनके हाथों से छिटक जाएगा।
कृष्ण प्रताप सिंह जी लिखते है कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इससे जुड़े मामलों के अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी की जगह
शुरुआती जांच की बात कही और दलित संगठनों ने इसको लेकर ‘भारत बंद’ का आह्वान किया किंतु सारे के सारे
राजनीतिक दल मौन की मुद्रा में सब कुछ को ऐसे देखते हे जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
दो अप्रैल 2018 के उस बंद के दौरान कई राज्यों में टकराव और हिंसा हुई तो गोदी मीडिया द्वारा आन्दोलन के दौरान हुई
हिंसा और टकराव को दलितों द्वारा ही की गई हिंसा कहकर प्रचारित किया गया और अनेक बेकसूर दलित-युवकों को
सलाखों के पीछे बन्द कर दिया उनमें से बहुत से आज भी जेलों में बन्द हैं। गुजरात के ही उना में दलित युवकों को बेरहमी
से पीटे जाने और लंबी मूंछें रखने के बहाने, नाम में उपनाम ‘सिंह’ लगाने या घुड़सवारी करने को भी उनपर अत्याचार
आज भी जारी है। ‘गवाह’ होने के बावजूद भी अनेक दबंग पुलिस कर्मी या यूँ कहें कि शासन-प्रशासन दलितों की दुर्दशा को
न समझ पाते हैं न उनके हक में कोई कार्रवाई ही करते हैं। जहां तक पुलिस कर्मियों की बात, उन्हें तो शासन के आदेशों का
ही पालन करना होता, इससे यह सिद्ध होता है कि शासन दलित और आदिवासियों के हक में काम करने का उपक्रम ही
नहीं करता।
पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हाथरस निवासी संजय जाटव को कासगंज के ठाकुर बहुल निजामपुर गांव में अपनी बारात
ठाकुर-बस्ती की निगाह से बचाने के लिए दूसरे रास्ते से ले जाना कुबूल नहीं हुआ तो कोर्ट-कचेहरी के चक्कर लगाने के
बावजूद जिलाधिकारी की मार्फत उन्हें ‘बीच का रास्ता’ ही मिल सका। ऐसी कितनी ही मिसालें हैं जहां दलितों को बेकसूर
होते हुए भी उन्हें सामाजिक न्याय से वंचित किया जा रहा है। यह सीधे-सीधे संविधान को अंगूठा दिखाने जैसा है। वैसे
राजनेता दलितों के घर खाना खाकर दलितों के पैरोकार होने का ढोल पीटते रहते हैं। बात तो जब बने कि जब दलितों के
पैरोकार होने का दावा करने वाले राजनेता दलितों को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं… ठीक उसी प्रकार जैसे कि वो
अपने सगे-संबन्धियों को खिलाते है… किंतु नहीं, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि उनकी दोगली मानसिकता उन्हें ऐसा
करने से रोक देती है। ऐसे नेता लोकतांत्रिक मूल्यों को सामाजिक चेतना का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? असंवैधानिक करार
दिये जाने के बावजूद भी छुआछूत के प्रति गैर-दलित समाज आज तक मूक क्यों बना रहता है…क्यों?
विदित हो कि आजादी मिलने से पहले देश की कुल आबादी के 16.6 प्रतिशत दलितों को अछूत कहा जाता था… उन्हें
महात्मा गांधी ने ‘हरिजन’ नाम दिया और अब सरकारी आंकड़ों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के नाम से जाना जाता
है। समयांतर में इनको ‘दलित’ नाम से जाना जाने लगा और आज जब ‘दलित’ वर्ग ‘दलित’ जैसे सम्बोधन के जरिए एक
होने लगा है (जैसे कि ‘हिन्दू’ जैसे शब्द के नाम पर एक हो गए) तो अब वर्तमान सरकार ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल पर
रोक लगाने पर उतारू है। मुम्बई हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से ऐसे समय में दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्देश
जारी किया जबकि दलित समाज अब ‘दलित’ शब्द को अपनी अस्मिता का प्रतीक मानकर संगठित होने का प्रयास कर
रहा है। यद्यपि आधुनिक पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शासन ने भारत की जाति व्यवस्था पर सत्ता ने दिन प्रति दिन
दिखावी किंतु दिखने में तगड़े हमले किए किंतु दलितों को इस व्यवस्था की बुनियादी औजार की तरह हमेशा ‘बचाकर’
रखा गया, ताकि हिंदू जाति की मनुवादी व्यवस्था फलती-फूलती रहे।
आज की तारीख में दलितों पर अत्याचार इसलिए भी कम या खत्म नहीं हो पा रहे क्योंकि जहां बाबासाहेब आंबेडकर का
सपना था कि आरक्षण की मदद से आगे बढ़ने वाले दलित दूसरे दबे-कुचले दलित वर्ग से बाहर लाने में मदद करेंगे, वहां
कुछ ऐसा सिलसिला बन गया है कि अब आगे बढ़ गए दलित खुद को अन्य दलितों से ऊंचे दर्जे का समझने लग गए हैं और
निचली पंक्ति के दलितों से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं और उनसे दूर होते नजर आते हैं। दूसरे-दलित समाज वो लोग जो
दलितों और आदिवासियों के वोट के बल पर चुनकर विधान सभा और संसद में आते हैं, वो दलित वर्ग के उत्थान के लिए
नहीं अपितु अपने राजनीतिक आकाओं के हक में काम करते हैं। अपनी कुर्सी बचाना उनका प्रथम लक्ष्य होता है। फलत:
शहरी और ग्रामीण दलितों की अवस्था में कोई वांछनीय उत्थान नहीं हुआ और दलितों को सरकारी नौकरियां और
रोजगार के दूसरे मौके कम होते जा रहे हैं।
इस संदर्भ में, नवभारत टाइम्स (24.12.2018) के अनुसार दलितों और आदिवासियों की स्थिति आज भी वहीं की वही
है। यूँ तो देश के राजनीतिक अजेंडे में दलित और आदिवासियों का स्थान बड़ा ऊंचा है। प्राय: हर राजनीतिक पार्टी उनकी
हालत सुधारने का वादा करती है या उनके साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाती है। लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति को
देखें तो निराशा होती है। आज भी यह तबका समाज में ‘नीच’ समझे जाने वाले पेशों में ही लगा है। अच्छी नौकरियां
उनके लिए सपना ही हैं। गैर कृषि श्रम से संबंधित जनगणना के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि निजी क्षेत्र में इनकी
उपस्थिति लगभग नगण्य है। कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेजर स्तर पर 93 प्रतिशत गैर दलित-आदिवासी लोग हैं। हां! सरकारी
नौकरियों में दलित – आदिवासियों की स्थिति कुछ-कुछ बेहतर कही जा सकती है, किंतु है नहीं। सरकारी स्कूलों में काम
करने वाले दलितों की संख्या 8.9 प्रतिशत और अस्पतालों में 9.3 प्रतिशत है। पुलिस में दलितों की संख्या 13.7 फीसदी है
जबकि आदिवासियों की तादाद 9.3 फीसदी है। (यहां अखबार द्वारा यह खुलासा नहीं किया गया हैं इनमें से कितने
प्रतिशत कर्मचारियों में कितने सफाई यानिकि क्लास फोर के कर्मचारी हैं… कितने प्रशासनिक पदों पर।) आज भी झाड़ू
लगाने और चमड़े के काम में दलितों की बहुतायत है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में चमड़े का काम करने वाले कुल
46000 लोगों में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 41000 है। उसी तरह राजस्थान में कुल 76000 सफाईकर्मी हैं
जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 52000 है। इनमें युवा अच्छी-खासी संख्या में हैं, जो इस बात का संकेत है कि
विकास की लंबी प्रक्रिया और सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिशों के बावजूद दलित जातियां शासन-प्रशासन के
रवैए के कारण अपना-अपना परंपरागत पेशा अपनाने को मजबूर हैं। जबकि हमारे राष्ट्र निर्माताओं का सपना था/है कि
जात-पांत के बंधन खत्म हो जाएं और हर नागरिक को तरक्की के समान अवसर मिलें। यह भी सोचा गया था कि जब
आर्थिक विकास तेज होगा और समाज में जनतंत्र का प्रसार होगा तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं रह जाएगा। हर
तरह के काम को बराबर सम्मान दिया जाएगा। किंतु ये दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हुए। सबकुछ इसके उलट हो रहा है। आज
21 वीं शताब्दी में भी तमाम नियम-कानून के बावजूद देश के दलित-आदिवासी दूसरे तबकों की तुलना में काफी पिछड़े
हुए हैं और उनका कई स्तरों पर उत्पीड़न जारी है।
ये कहना बेजा नही कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान तो किया
गया किंतु दलित-दमित-आदिवासियों की शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण से दलित और आदिवासी
बेहतर नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता हासिल ही नही कर पाते क्योंकि वे उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते। गांवों में
किसी तरह सरकारी स्कूलों में ये प्राथमिक शिक्षा हासिल कर भी लेते है तो गरीबी के कारण उनमें से ज्यादातर आगे नहीं
पढ़ पाते। आज ऊंचे दर्जे की पढ़ाई छोड़ने की दलितों की दर, गैर दलितों के मुकाबले दोगुनी है। इसमें शिक्षा का
निजीकरण महती भूमिका निभा रहा है। मंहगी शिक्षा का भार गरीब दलित और आदिवासी अभी उठाने की हालत में
नहीं है और सरकारी स्कूलों/कालिजों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उदारीकरण यानि कि उद्योग और
व्यावसाय के निजीकरण के कारण सरकारी नौकरियां कम हुई हैं। निजी क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, उनके अनुरूप शिक्षा और
तकनीकी निपुणता हासिल करना इन जातियों के लिए बेहद मुश्किल है। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को योग्य न होते
हुए भी फेल न करना भी दलितो और आदिवासियों के साथ एक साजिश का हिस्सा लगती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में
बड़ी नौकरियों के दरवाजे इनके लिए नहीं खुल रहे। कहना अतिशयोक्ति नहीं कि आजादी के 70 साल बाद भी दलित और
आदिवासियों की आर्थिक/सामाजिक अवस्था में कुछ भी अंतर नहीं आया। सब कुछ पहले जैसा ही है। हां! भौगोलिक स्तर
जो भी बदलाव हुए हैं, उनके चलते दलित और आदिवासियों में अंतर देखने को मिलता है… अन्यथा नहीं।
सरकार को जान लेना चाहिए कि सिर्फ नारों से दलित-आदिवासियों का उत्थान नहीं होने वाला। सरकार को वे तमाम
प्रयास करने होंगे जिनसे दलित व आदिवासियों के बच्चे उच्च शिक्षित और निपुण बन सकें। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार
इस सुझाव पर अमल करती है तो आरक्षण को लेकर रोज का उठने वाला आरक्षण का शौर भी कम हो जाएगा। या फिर ये
कि समाज की तमाम जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय ताकि देश में आरक्षण
कोई प्रश्न ही न रह जाए।
