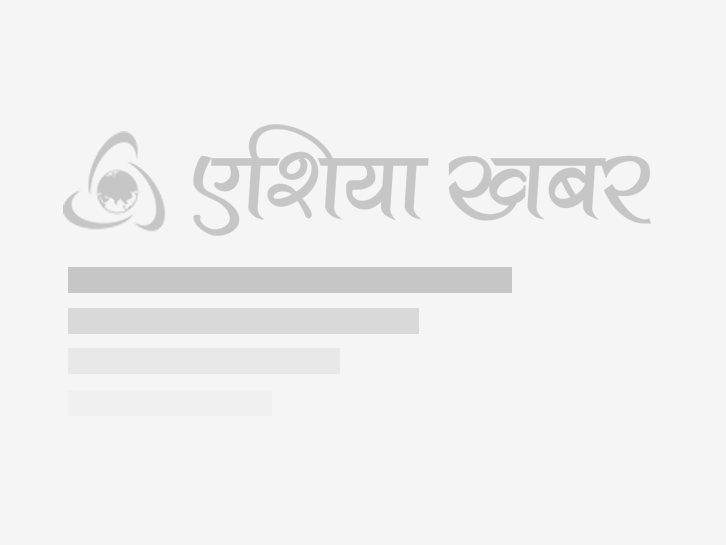
जनता दल सेक्युलर नेता व कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी और कांग्रेस नेता व उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरा के बंगलुरू शपथ ग्रहण समारोह पर बुधवार को पूरे देश की नजर गड़ी रही, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले दिग्गज राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के राजनेताओं के हावभाव और स्वभाव के विपरीत दिखाई जाने वाली आपसी घुलनशीलता से केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार और कथित साम्प्रदायिक पार्टी बीजेपी विरोधी धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन की दशा और दिशा तय होना था।
लेकिन जिस तरह से इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने कुछ नेताओं के दिलेर स्वभाव ने इस बात की पूरी उम्मीद जगाई और कुछ नेताओं के संकीर्ण मिजाज ने इन तमाम बंधी-बंधाई उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उसकी विस्तृत चर्चा करने से पहले इस पूरी मुहिम की प्रासंगिकता के ऊपर जो कतिपय सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उसके विभिन्न पहलुओं की भी निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है ताकि इस महामोर्चा के भविष्य पर अमूमन छाए रहने वाले संशय के बादल कुछ छंट सकें।
ऐसा इसलिए कि 2015 में मोदी-बीजेपी की धुर विरोधी बिहार की महागठबंधन सरकार के एक ऐसे ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह और उसमें शिरकत करने वाले, किन्हीं कारणों वश ना करने वाले राजनेताओं का नजीर सबके सामने है। तब भले ही मंच पर सोनिया गांधी और मायावती की कमी सबको खली थी, लेकिन उसके बाद गठबंधन के ही साथी दलों में उभरे अंतर्विरोध जिसमें जदयू के खिलाफ राजद-कांग्रेस की भूमिका किसी सियासी खलनायक से कम नहीं रही, से परेशान जदयू ने कैसा विस्मयकारी निर्णय लिया और उस भव्य समारोह के मुखिया नीतीश कुमार ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए कैसे उसी बीजेपी के समक्ष घुटने टेके, जिसके खिलाफ बड़ा और यादगार जनादेश हासिल किया था। जबकि जदयू-बीजेपी पहले भी लंबे अरसे तक एक दूसरे के अभिन्न सहयोगी थे, और बदली हुई परिस्थितियों के बाद आज भी हैं!
शायद यह भी एक वजह है कि इस बात की कोई नही गारंटी नहीं दी जा सकती कि कर्नाटक में इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा और मौजूदा महागठबंधन सरकार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के मुखिया एचडी कुमारस्वामी भविष्य में निज स्वार्थों का दम घुटते देख पलटी नहीं मारेंगे! क्योंकि जेडीयू की तरह जेडीएस भी विवादास्पद जनता दल के विखंडित होने से ही बना है। सर्वाधिक दिलचस्प बात तो यह कि नीतीश कुमार की तरह ही कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ पहले सत्ता सुख भोग चुके हैं। लिहाजा बेहतर अवसर मिलते ही कब पलटी मार देंगे, निश्चयपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस बारे में कोई भी सुनिश्चित सोच बनानी किसी बचकानी बात जैसी होगी जिसका कोई भविष्य नहीं होगा।
हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति सम्भावनाओं का खेल है। पारस्परिक स्वार्थों का समुच्चय है। और सबसे बढ़कर सदनीति नहीं बल्कि अनैतिक अंकगणित का खेल है। हमारे राजनेताओं का सियासी अतीत और वक्त-वक्त पर उभरकर सबके सामने आया उनका विरोधाभाषी चरित्र भी इसी बात की चुगली करता है। इसलिए मोदी सरकार और बीजेपी नीत एनडीए सरकार की थोड़ी सी भी लापरवाही या रणनीतिक चूक उस पर भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसी ही बात है कि भारतीय राजनीति के सियासी नक्शे से तेजी से गायब होता जा रहा विपक्ष तेजी से गोलबंद होकर बीजेपी पर हमला बोलने की जिस ताक में था, उसका मौका कुछ उपचुनावों के बीजेपी विरोधी रुझानों के साथ साथ कर्नाटक के त्रिशंकु जनादेश ने दे दिया। यहां पर कांग्रेस ने जैसी उदारता दिखाई है, वह सिलसिला यदि जारी रहा तो संघ-बीजेपी दोनों की मुश्किलें निकट भविष्य में बढ़ सकती हैं।
आप मानें या न मानें, लेकिन जिस मंच पर जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस आलाकमान और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, बसपा नेत्री और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित सिंह, दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव, टीडीपी नेता व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तृणमूल कांग्रेस नेत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और माकपा नेता सीताराम येचुरी जैसे दिग्गज राजनेता मौजूद हों, वहां पर ओडिशा के मुख्यमंत्री व बीजद नेता नवीन पटनायक की गैर मौजूदगी के अलावा सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की नुमाइंदगी यदि उनके पुत्र व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राजद सुप्रीमो लालू यादव का प्रतिनिधित्व यदि उनके पुत्र व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करें तो कितना मनहूस लग रहा होगा, सभी जानते हैं। इसलिए सवाल फिर वही कि क्या यह स्थिति किसी सफलता की गारंटी बन सकेगी?
यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जेएमएम नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला, द्रमुक नेता डी राजा, तमिल नेता कमल हासन, जेडीएस नेता दानिश अली आदि राजनेता जो कि मंच पर बेहद कम घुले-मिले, यदि पीएम मोदी का विकल्प बनने की बात सोचें तो या तो ये नादान हैं या फिर इनको प्रोजेक्ट करने वाले विकल्पहीन! क्योंकि मोदी का विकल्प कौन होगा और कितने दिन तक रह पाएगा? यह असली सवाल है, जिसका स्प्ष्ट उत्तर देने से प्रायः सभी नेता बच रहे हैं। सिर्फ ममता बनर्जी हैं जो लोगों को यह समझा रही हैं कि राहुल गांधी उनके नेता नहीं हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि वो इस मसले पर मुखर हैं और अकेली भी नहीं होंगी, ऐसी अटकलें हैं।
यही नहीं, विपक्षी एकता के मायने क्या हैं? महज मोदी विरोध के आधार पर ये कितने डग भर पाएंगे? क्या अपने-अपने राज्यों की परस्पर धुर विरोधी पार्टियां पहले लोकसभा चुनाव और फिर राज्यसभा चुनाव आपस में मिलजुल कर बिना विवाद किए लड़ पाएंगी? नेतृत्व-दिशा-सेवाभाव की किल्लत झेल रही कांग्रेस क्या यूपी-बिहार-कर्नाटक की तरह ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में छोटे भाई की भूमिका स्वीकार करेगी। क्या कर्नाटक मधुर मिलन के बाद धर्मनिरपेक्ष दलों की आपसी प्रतिद्वंद्विता पर विराम लग जायेगा? या फिर सामाजिक न्याय की पैरोकारी करने वाले दल अब व्यक्तिगत टकराव के बावजूद आपसी मारामारी से परहेज करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके सकारात्मक जवाब से ही महागठबंधन के दीर्घायु होने के आसार हैं, अन्यथा इनके अल्पायु होने की कहानी घर-घर में सुनी-सुनाई जाती है जो कि देश का सियासी दुर्भाग्य समझा जाता है।
इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस शपथ ग्रहण समारोह में सात राज्यों के तकरीबन 15-20 वैसे नेता जुटे, जिनकी आपसी प्रतिस्पर्द्धा जगजाहिर है। फिर भी पहली बार उनके जुटने से इस बात को बल मिला है कि पीएम नरेंद्र मोदी विरोधी और बीजेपी के खिलाफ जिस देशव्यापी महामोर्चा की बात चली है वह अनायास नहीं बल्कि तेजी से जनाधार और सत्ता खो रही कांग्रेस की किसी सुविचारित रणनीति का परिणाम है जिसके पत्ते वह धीरे-धीरे खोलेगी। दूसरी तरफ उसको शह देने वाले क्षेत्रीय दल भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि गैर भाजपा संघीय मोर्चा बनाया जाए या फिर कांग्रेस की अगुवाई वाला बीजेपी विरोधी मोर्चा। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ माकपा ने तो दो टूक मोर्चा भी खोल दिया है। सवाल यह भी है कि 1998-99 में एनडीए को एकसूत्र में पिरोने वाले जार्ज फर्नांडिस और 2004 में यूपीए को एकधागे में जोड़े रखने वाले हरकिशन सिंह सुरजीत का स्थान इस बार कौन लेगा, क्योंकि शरद यादव या शरद पवार में वो दमखम नजर नहीं आता। यदि चंद्रबाबू नायडू प्रत्यक्ष रूप से या फिर लालू यादव परोक्ष रूप से इस मुहिम की कमान संभाले, तब भी कुछ बात बन सकती है।
यही वजह है कि तमाम नानुकुर के बावजूद भी क्षेत्रीय नेतागण इसे पूरे दमखम के साथ साकार करेंगे, क्योंकि अब देश और लोकतंत्र को खतरा हो या न हो, लेकिन इनके सियासी और व्यक्तिगत दोनों वजूद को खतरा उत्पन्न हो चुका है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये भले ही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करके किसी के नेतृत्व में जुटते हैं और जब इनके व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि नहीं होती है और छिपे एजेंडे की बात नहीं बनती है तो इनके टूटने, टूटकर बिखरने और यहां तक कि सत्तालोभ वश बीजेपी की शरण में जाकर अपने ही साथियों को नीचा दिखाने में देर नहीं लगती, यही राष्ट्रीय चिंता और विमर्श दोनों का विषय है।
बहरहाल, इस भव्य समारोह के फोटो सेशन से अरविंद केजरीवाल का ओझल रहना, ममता बनर्जी द्वारा राहुल गांधी को पूरा महत्व नहीं देना, उत्तर और दक्षिण भारत के नेताओं का अलग-थलग रहना तथा पद व राजनीतिक कद वाले नेताओं के अनमने चेहरों को देखकर तो यही महसूस हुआ कि इनकी कटुता जो इस मंच पर आते ही खत्म हो जानी चाहिए थी, कहीं न कहीं दबी हुई है जो किसी भी सियासी जख्म के मिलते ही उभर सकती है। बावजूद इसके, इनमें 2019 में किंगमेकर नहीं किंग बनने की जो स्पष्ट ललक दिखाई दे रही है, उससे 2019 का लक्ष्य भले ही कठिन लगे या नहीं, लेकिन उसके बाद का सियासी रास्ता बहुत दुर्गम होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
