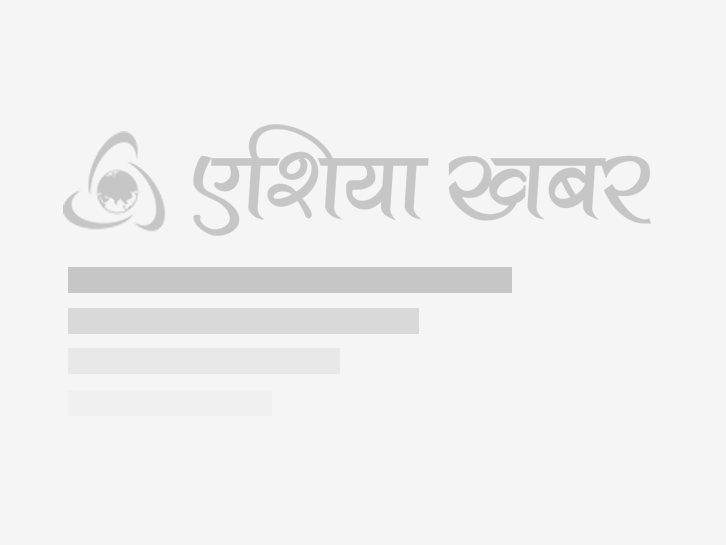शिक्षा जिस तेजी से अपना चोला बदल रही है उस रफ्तार से हमारी चिंतन शैली, विमर्श की गति नहीं बदल रही है। शायद हम शिक्षा के बदलते मिज़ाज को पहचानने में भूल कर रहे हैं। आज भी हम 1990 और 2000 के दशक में ठहर कर शिक्षा को देख और जी रहे हैं। यही कारण है कि हमारे लिए महज बीए, बीएस सी, बी. कॉम जैसे पारंपरिक कोर्स ही लुभा रहे हैं। हालांकि अब के बच्चे और अभिभावक भी करवटें तो ले रहे हैं लेकिन शिक्षा के बाजार को समझने में पीछे हैं। क्योंकि यदि बच्चों की परीक्षा की प्रकृति को देखें तो बड़ी तेजी से एक परिवर्तन देखा जा सकता है कि बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग के अलावा लॉ आदि में भी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। लेकिन यह तेजी और रूचि समय और बाजार की मांग की दृष्टि से समयानुकूल नहीं माना जा सकती। शिक्षा की दुनिया को समझना हो तो कई बार भारत के बाहर नज़रें डालनी पड़ेंगी। जहां शिक्षा महज स्नातक और परास्नातक तक महदूद नहीं रही। बल्कि शिक्षा पारंपरिक चोले से बाहर निकल कर खेल कूद रही है।
हर साल गर्मी की छुटि्टयों में शिक्षा एक प्रकार से मैला और मेले की ढर्रे पर ढलती नजर आएगी। इधर स्कूलों की छुट्टी हुई नहीं उधर गतिविधियों का बाजार अपना सामान बेचने लगता है। गली गली, मुहल्ला मुहल्ला आपके बच्चे को एक बेहतर और चरफर इंसान बनाने के दावे करने लगता है। उनके तो दावे यह भी होते हैं कि हम आपके बच्चे को एक्टर, डांसर, थिएटर पर्सन और न जाने किन किन निर्माणों के ख्वाब दिखाने लगते हैं। गोया बच्चे न हुए मिट्टी के लोदे हो गए। जो स्कूल साल भर में नहीं गढ़ पाए वे महज एक या डेढ़ माह में कर दिखाएंगे। हालांकि समय और श्रम पर भी निर्भर करता है कि किस बच्चे में कौन सी क्वालिटी डेवलप की जा सकती है। जो बच्चा एकदम गुम्मा रहता है। मुंह ही नहीं खोलता ऐसे बच्चों के अभिभावक चिंतित रहते हैं कि वह बोलता नहीं। गतिविधियों में भाग नहीं लेता आदि। कैसे भी उनका बच्चा और बच्चों की तर्ज पर शरारतें करने लगे, उसका कम्यूनिकेशन स्किल बेहतर हो जाए। मालूम नहीं यह तो अभिभावक ही बेहतर बता सकते हैं कि इन आधी मई और जून के माह में उनके बच्चों की कितनी ग्रूमिंग हो पाती है। कितनी अपेक्षाएं पाली होंगी और उनमें से कितना और किस प्रकार का परिवर्तन हो सका।
जो भी हो आपका बच्चा डांस करना सीख पाए या नहीं लेकिन बाजार ने आपको सपने तो बेच ही दिए। एक सवाल यह भी उठता है कि नब्बे के दशक में इस प्रकार की समर कैम्पों की बाढ़ नहीं आई थी। बच्चे इन छुटि्टयों में मौज मस्ती किया करते थे। दादा-दादी, नाना−नानी के घर या फिर कहीं घूम−टहल आते थे। तब क्या बच्चों की ग्रूमिंग नहीं होती थी। क्या तब के बच्चे घर−घुस्सा हुआ करते थे? आदि ऐसे सवाल हैं जिन पर हम आज की बलबलाती गतिविधियों के उफान को समझ सकेंगे। ऐसा कत्तई नहीं है कि तब के बच्चों ने अपने जीवन में मुकाम नहीं हासिल किया। या वे बच्चे इंट्रोवर्ट रहे गए। यदि ऐसा होता तो हमें बेहतर पत्रकार, लेखक, वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट, वक्ता नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ मसला यह भी है कि क्या बच्चों की सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी स्कूल और शिक्षकों की नहीं होती है? क्या शिक्षक और स्कूल सिर्फ टेक्स्ट बुक, करिकूलम आदि को पूरा कराने की जिम्मेदारी के आधार पर अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं। क्योंकि शिक्षा का तो एक उद्देश्य और शायद मुख्य उद्देश्य बच्चे को एक सफल और सार्थक नागरिक बनाना है। यदि हमारी स्कूली शिक्षा इस जवाबदेही में पिछड़ती है तो हम कहीं न कहीं प्रकारांतर से बाजार को ऐसी गतिविधियों एवं समर कैंपों को बढ़ावा ही दे रहे हैं।
हमारे बच्चे सिर्फ समर कैंपों के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। उन्हें इन समर कैंपों के तामझाम से बाहर निकालना होगा। क्योंकि बच्चों की ग्रूमिंग में इस प्रकार की गतिविधियों की भूमिका होती है लेकिन इतनी भी नहीं कि वो स्कूली परिवेश पर भारी पड़ने लगे। हमें आज नहीं तो कल अपनी स्कूली शिक्षा को ही दुरूस्त करना होगा। विश्व के अन्य कोनों में शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या क्या और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें संज्ञान में लाना होगा। शायद यही वजह रही हो और थी भी कि समय समय पर शैक्षिक समझ बनाने के लिए शिक्षाकर्मी, शिक्षक, मंत्री आदि विदेशों का दौरा करते हैं ताकि वहां की शिक्षा और स्कूली तंत्र को समझा जा सके और उसे भारतीय परिवेश में मुकम्मल कैसे बनाया जाए इस पर एक रोड़मैप बनाया जाए। लेकिन क्या हक़ीकत से हम मुंह फेर सकते हैं कि इस प्रकार की शैक्षिक यात्राएं शैक्षिक−समझ से ज़्यादा व्यक्तिगत विकास और ग्रूमिंग में जाया हो जाती हैं।
दिल्ली सरकार ने यही कोई तीन साल पहले पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छांटकर 200 मेंटोर शिक्षक का दल बनाया था। उनमें से कुछ को बाहर भी ले जाया गया। ताकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाई जा सके। उस प्रोजक्ट का क्या हुआ? क्या हुआ उन तमाम कार्यशालाओं का जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शिक्षा में पैसे खर्च करने को हर कोई तैयार है बस कमी इस बात की है कि हमारे पास काम करने की ललक, क्षमता, दक्षता, टाइम मैनेजमेंट और समय पर अपने लक्ष्य को पाने की तड़प नहीं है।
आज की तारीख में उपयुक्त कैंडिडेट पाना बेहद चुनौतियों भरा काम है। यदि आप बाजार में योग्य उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं तो महज डिग्रीधारियों से आपका काम नहीं चलने वाला। डिग्रियां सभी के पास हैं। कोई नेट, पीएचडी, तो कोई एम एड भी हैं। लेकिन जब हक़ीकत से रू ब रू होते हैं तब घोर निराशा होती है। क्योंकि डिग्री तो है लेकिन डिग्री के अनुरूप उनके पास न तो समझ है और न ही अपेक्षित योग्यता। कहने को पोस्ट ग्रेजुएट हैं। प्रशिक्षकीय डिग्री भी हासिल की हुई है। जब आप ऐसे कैंडिडेट की प्रोफाइल से गुज़रते हैं तो एक उम्मीद बंधती है कि कम से कम एक तो ऐसा प्रतिभागी मिला जो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है। लेकिन जब उससे बातचीत करते हैं, कुछ गहरे में उतरते हैं तब हैरानी इस बात की होती है कि डिग्री अपनी जगह है और विषयी समझ बिल्कुल दूसरे छोर पर है। तब कई बार चिल्लाने का मन करेगा कि यह कैसी पढ़ाई है? कैसी तालीम दी जा रही है जिसमें डिग्रियां तो दी जा रही हैं किन्तु डिग्री के स्तरीय ज्ञान और समझ नहीं है। मालूम हो कि दिल्ली विश्ववदि्यालय में बीए या एमए पर जितने पैसे खर्च हो जाते हैं उससे कम से कम चार गुणा अधिक खर्च पर निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय में इन्हीं डिग्रियों को हासिल करने के लिए हमारे आज के युवा भीड़ लगा कर खड़े हैं। कहीं भी योग्यता और समझ की चिंता नज़र नहीं आती।
हाल ही में विभिन्न पोस्ट के लिए कैंडिडेट के इंटरव्यू में बैठने का मौका मिला। बॉयोडेटा क्या ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। बॉयोडेटा को अच्छे से मैनेज कर और प्रेजेंटेबल भी बनाया गया था। जिसमें तमाम डिग्रियां, डिप्लोमा, विभिन्न सेमिनारों, वर्कशॉपों की लंबी सूची बनाई गई थी। उन बॉयोडेटा में कई तरह की हॉबी का भी जि़क्र था। प्रसन्नता इस बात की थी कि कम से कम संस्थान को एक योग्य और सही कैंडिडेट मिल सकेगा। जो आगे चल कर संस्थान के मिशन, विज़न और लक्ष्य को हासिल करने में अपनी समझ और योग्यता का इस्तमाल करेंगे। लेकिन जब बातचीत का सिलसिला निकला तो एक एक कर पिछड़ते चले गए। मुझे उनके पिछड़ने का दुख जितना नहीं था उससे कहीं ज़्यादा उनके पिछड़ने की वज़हों की पहचान कर कोफ्त से भर रहा था। अफसोस इस बात का था कि जिन कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की पहचान अपनी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए थी वहां से ऐसे ऐसे छात्र बाजार में आ रहे हैं। ताज्जुब तो इस पर हुआ जब उनकी आंखों में इसका इल्म भी नहीं दिखा कि उन्हें दुख है कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं लगा कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसे वे समझ भी नहीं पा रहे हैं। साहित्य में भाषा व शब्द की तीन ताकतों की चर्चा होती है− अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। वे प्रतिभागी इन तीनों के भाषायी जादू से बेखभर थे। जबकि वे जिन पोस्ट के लिए आए थे वह भाषा विशेषज्ञ के लिए ही था।
यदि आप शिक्षा जगत में हैं। उसमें भी स्कूली शिक्षा से आपका साबका रहा है तो आपसे इतनी तो अपेक्षा की ही जा सकती है कि आपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का नाम सुना हो, आपने कभी भूलवश ही सही इस एनसीएफ को उलट पलट कर देखा हो, या फिर कहीं किसी से चर्चा सुनी हो या फिर अखबारों, पत्रिकाओं में आलेख ही पढ़े हों। यदि इंटरव्यू बोर्ड इसकी उम्मीद रखता है कि आपको एनसीएफ के बारे में मालूम होना चाहिए तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ उत्तरों को पढ़ और सुनकर शिक्षण प्रोफेशन से ही विश्वास उठने सा लगा। सुबह उठकर अपने बड़ों का प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, स्कूल नहा धोकर जाना चाहिए यह एनसीएफ भाषा−शिक्षण संबंधी सिफारिश करता है। शिक्षा से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इन उत्तरों पर हंसी से ज़्यादा उन संस्थानों से शिकायत होगी जहां से ऐसी समझ लेकर बच्चे बाजार में आ रहे हैं।
दरअसल शैक्षिक संस्थान भी आज की तारीख में महज बाजार को तवज्जो देते हुए कोर्स और कोर्स के खेवनहारों को रखते हैं। जहां की फैकेल्टी स्वयं डिमोटिवेटेड होगी, खुद ने कभी शोध पत्र न लिखे हों, जिनकी खुद की स्कूली समझ पतली है वे किस प्रकार की शैक्षिक समझ बच्चों में संक्रमित करेंगे इसका अनुमान लगाना ज़रा भी कठिन कठिन नहीं है। जब से बहुवैकल्पिक सवालों और परीक्षा का ढर्रा निकल और चल पड़ा है तब से विषयनिष्ठ समझ दूर की कौड़ी होती गई है। भाषा और शिक्षा शास्त्र में तो और स्थितियां चिंताजनक होती गई है। बच्चों को पांच वाक्य लिखने को दिया जाए तो उसमें साठ से सत्तर फीसदी ग़लतियां मिलेंगी जो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से उचित नहीं है। वहीं तथ्य और समझ के स्तर पर भी उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।