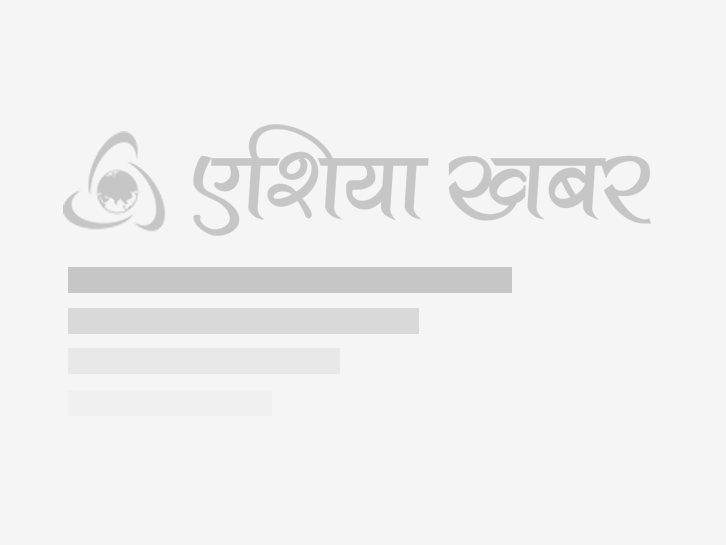
-विकास सारस्वत-
तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई आलोचना ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच फिर एक बार टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से विधानसभा में पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल की सहमति रोके रखने का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था।
अपने अनूठे निर्णय में न्यायालय ने न सिर्फ इन लंबित विधेयकों को राज्यपाल की सहमति के बिना ही मंजूर घोषित किया, बल्कि राज्यपाल के लिए तीन माह के भीतर ऐसे बिलों को वापस विधानसभा भेजने अथवा राष्ट्रपति के समक्ष विचार हेतु प्रेषित करने की समयसीमा भी निश्चित कर दी।
इतना ही नहीं, न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया कि उन्हें राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की निष्क्रियता के खिलाफ राज्य अदालत जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राज्यपाल की शक्तियों का अधिग्रहण कर विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप तो किया ही, संघीय ढांचे में केंद्र की ओर शक्ति के झुकाव को भी कुंद किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसी पर आपत्ति जताई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा के घर मिले अधजले नोटों के मामले में कोई एफआइआर न दर्ज किए जाने पर भी प्रश्न खड़े किए।
समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्रीय कानूनों की सर्वोच्चता, सातवीं अनुसूची में शामिल होने से रह गए अवशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार ऐसे कुछ प्रविधान हैं, जो केंद्र की सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं।
अनु. 355 एक ऐसी शासकीय व्यवस्था की कल्पना करता है, जिसमें केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का भार होता है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व का पालन संवैधानिक प्रविधानों के अनुरूप करें। इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति की अपेक्षा राज्यपाल के पास कहीं अधिक और वास्तविक शक्तियां होती हैं।
कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने या फिर असंवैधानिक कार्यकलापों का मामला संज्ञान में आने पर वह विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु राज्यपाल के समक्ष आए विधेयकों को अनुमति देने या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित रखने की कोई सीमा नहीं है।
जिन 10 विधेयकों को लेकर राज्य सरकार ने याचिका दायर की, उनमें एक विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन का अधिकार राज्यपाल से हटाकर मंत्री परिषद को देने की बात करता है। ऐसे में याचिका का दायरा सीमित कर विषय केंद्रित किया जा सकता था, परंतु राज्यपाल और राष्ट्रपति, दोनों के लिए प्रत्येक विधेयक को अनुमति की समयसीमा में बांधे जाने ने न केवल राज्यपाल के पद को कमजोर किया, बल्कि राज्य को एक तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षी अधीनता से मुक्त कर दिया।
ऐसी व्यवस्था के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। नागरिकता संशोधन और वक्फ कानून के विरोध में पारित प्रस्तावों के जरिये विभिन्न विधानसभाएं कई बार अपने भयावह मंतव्यों को प्रकट कर चुकी हैं। तमिलनाडु विधानसभा तो कोयंबटूर बम धमाकों में निरुद्ध विचाराधीन कैदी अब्दुल नसीर मदनी की रिहाई का प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राष्ट्र की एकता और अखंडता को दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है।
हाल में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा है। मजहबी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था तय करने वाला यह विधेयक पूरी तरह गैर संवैधानिक है, पर शीर्ष अदालत का हालिया निर्णय राष्ट्रपति को यह विधेयक पास करने के लिए बाध्य करेगा।
ऐसी सूरत में इसके निस्तारण का एकमात्र उपाय फिर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे के रूप में ही होगा। यह संकट उस बढ़ती प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसमें न्यायपालिका विधायिका के ऊपर एक सुपर वीटो के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। चाहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को रद करना हो या कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक, विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का अतिक्रमण जारी है।
पिछले कुछ समय से संसद द्वारा पारित करीब-करीब हर विधेयक का न्यायपालिका द्वारा तुरंत संज्ञान लेना भी एक परिपाटी बन गई है। इसी कारण राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के एक सप्ताह बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हो गई। लंबे समय तक संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को उपयोग में लाने के बाद अब अनुच्छेद 142 न्यायिक अतिक्रमण का आधार बन गया है। तमिलनाडु के मामले में भी न्यायालय ने इसी का सहारा लिया है।
अनु. 142 वह असाधारण प्रविधान है, जो सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में ‘पूर्ण न्याय’ प्रदान करने की गुंजाइश देता है, जहां कोई प्रत्यक्ष कानूनी उपाय मौजूद न हो। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संघीय कार्यपालिका को किसी विधेयक की वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए तथा उसे अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय भेजना चाहिए।
इस हिसाब से विभिन्न राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित प्रत्येक विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना न सिर्फ अव्यावहारिक है, परंतु स्वयं न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रण करने वाला न्यायिक तख्तापलट भी है।
2015 में एनजेएसी रद होने और 2023 में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर न्यायालय ने अनु. 142 के उपयोग की चेतावनी दी थी, पर जस्टिस वर्मा के घर अधजले नोटों की बरामदगी को उसने अनु. 142 के प्रयोग के लायक नहीं समझा। उपराष्ट्रपति की पीड़ा जायज है। यदि न्यायिक अतिक्रमण पर रोक नहीं लगी तो भारतीय लोकतंत्र न्यायिक अधिनायकवाद का रूप ले सकता है।
