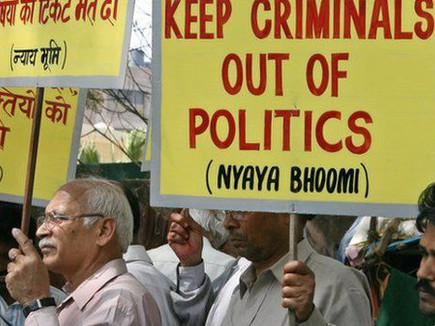
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों केंद्र सरकार को सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सर्वोच्च अदालत की इस पहल को सराहनीय माना जा रहा है, पर इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल और मुद्दे भी हैं, जो दशकों से अनुत्तरित हैं। पहला अहम सवाल तो यही कि क्या गवाहों की सुरक्षा के बिना अत्यंत प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जारी किसी मुकदमे को उनकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जा सकता है? क्या अधिकतर विवेचना अधिकारियों की मौजूदा लचर कार्यशैली में सुधार के बिना सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य पूरा हो पाएगा? क्या नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग पर रोक से संबंधित खुद के 2010 के आदेश को पलटे बिना सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का सकारात्मक असर हो पाएगा?
देश के राजनीतिक तंत्र को दागियों से मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ अन्य दिशा-निर्देश भी आने चाहिए। यह ध्यान रहे कि पुलिस हत्या जैसे संगीन जुर्म के मामले में भी जितने लोगों के खिलाफ अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करती है, उनमें से सिर्फ 10 प्रतिशत आरोपितों को ही सजा हो पाती है। दुष्कर्म या बलात्कार के मामले में यह प्रतिशत सिर्फ 12 है। अधिकतर मामलों में गवाह अदालत में जाकर पलट जाते हैं, क्योंकि वे अपार राजनीतिक, प्रशासनिक और बाहुबल की ताकत से लैस आरोपियों के सामने टिक नहीं पाते हैं।
अमेरिका और फिलीपींस सहित दुनिया के कई देशों में गवाहों की सुरक्षा के लिए कई कानूनी और अन्य उपाय किए गए हैं। अमेरिका में 8500 गवाहों और उनके 9900 परिजनों को 1971 से ही मार्शल सर्विस सुरक्षा दे रही है। खुद अपने यहां सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह गवाहों की सुरक्षा के उपाय करे। 1958 में विधि आयोग ने भी गवाहों की सुरक्षा के उपाय करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे, पर कुछ नहीं हुआ। इस तरह की अनेक खामियों के कारण आपराधिक मामलों में पूरे देश में सजा का औसत प्रतिशत सिर्फ 45 है। 1953 में यह प्रतिशत 64 था। सीबीआई थोड़ा बेहतर नतीजे जरूर देती है, फिर भी विकसित देशों के मुकाबले यहां की स्थिति दयनीय ही कही जाएगी। अमेरिका में सजा का प्रतिशत 93 है, तो जापान में 99 प्रतिशत। अपने देश में सत्तर के दशक से ही सजा के प्रतिशत में गिरावट शुरू हो गई थी।
यह संयोग नहीं है कि राजनीति के अपराधीकरण का भी वही शुरुआती दौर था। जिन राज्यों में राजनीति का अपराधीकरण अधिक हुआ है, उनमें सजा का प्रतिशत भी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। न सिर्फ गवाह ताकतवर आरोपी के प्रभाव में आ जाते हैं, बल्कि अनेक जांच अधिकारी भी रिश्वत के प्रभाव से बच नहीं पाते। वैसे भी पुलिस में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए गवाहों की सुरक्षा के साथ-साथ मामले की जांच के काम में लगे अधिकारियों पर भी नजर रखने का विशेष प्रबंध करना पड़ेगा। बेहतर तो यह होगा कि धनवान लोगों के केस देखने वाले जांच अधिकारियों पर भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते नजर रखें।
समयसीमा के भीतर सांसदों-विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के मामले में कोई भी ढील आरोपितों को मदद पहुंचाने के समान ही होती है। सजा के बाद पूरे जीवन में फिर कभी चुनाव नहीं लड़ने के प्रावधान का भी सवाल सामने है। दरअसल ऐसा किए बिना लोकतंत्र को इस गंदगी से मुक्त नहीं किया जा सकता, किंतु इस पर केंद्र सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया से कोई खास उम्मीद नहीं बंधती, क्योंकि आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिकाकर्ता की मांग पर सरकारी वकील ने गत एक नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ‘इस पर विचार हो रहा है। सरकारी सूत्रों ने अलग से बताया कि इस पर तो राजनीतिक दलों में आम सहमति की जरूरत पड़ेगी।
समस्या है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों में आमतौर पर कोई सहमति नहीं बन पाती, क्योंकि यह सांसदों के वेतन-भत्ते और सुविधाएं बढ़ाने का मामला तो है नहीं! उस पर तो आम सहमति कायम होने में कभी कोई देर नहीं होती। इसी आम सहमति के चक्कर में राजग सरकार को 2002 में फजीहत झेलनी पड़ी थी। क्या राजग सरकार मौजूदा मामले में भी उसकी पुनरावृत्ति चाहती है? पता नहीं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में सख्त आदेश देकर केंद्र सरकार के उस निर्णय को बदल दिया था जिसके तहत केंद्र सरकार ने उम्मीदवारों के बारे में निजी सूचनाएं देने की पहले मनाही कर दी थी। उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक मुकदमे और संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी तभी हो सका था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार को स्पष्ट आदेश दिया। उससे पहले केंद्र सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं थी। केंद्र सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पसंद नहीं किया था। अधिकतर राजनीतिक दल भी नहीं चाहते थे कि ऐसी व्यक्तिगत सूचनाएं जगजाहिर की जाएं। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार ने तब राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा दिया। बाद में उसे संसद ने पारित करके कानून का भी दर्जा दे दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। उसके बाद ही ये सूचनाएं चुनाव में नामांकन पत्र भरने के साथ उम्मीदवार देने को बाध्य हो रहे हैं। यानी जिस देश के अधिकतर राजनीतिक दल और नेतागण अपने बारे में सामान्य सूचनाएं भी सार्वजनिक करने को तैयार नहीं, वे अपराधियों को चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए रोकने के लिए खुद कोई कानून बनाने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा फिलहाल लगता नहीं है।
याद रहे कि जनहित याचिकाकर्ता ‘लोक प्रहरी और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई है कि सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी या जज को सजा हो जाए तो उन्हें फिर से नौकरी नहीं मिलती। यह समानता के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है कि सजा की अवधि पूरी कर लेने के छह साल बाद नेता फिर से चुनाव लड़ने के योग्य माने जाएं। उम्मीद है कि 13 दिसंबर को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार आजीवन प्रतिबंध के मामले में अपनी अंतिम राय सर्वोच्च न्यायालय को बता पाएगी। चुनाव आयोग तो ऐसे प्रतिबंध के पक्ष में पहले से ही है। खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना होगा कि 2010 के उसके ही एक निर्णय का आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया पर कैसा असर पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मई 2010 में यह कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना उसका न तो नार्को एनालिसिस टेस्ट हो सकता है और न ही ब्रेन मैपिंग। उस पर झूठ पकड़ने वाली मशीन का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब इस पर विचार करने की जरूरत है कि इस आदेश के बाद जांच अधिकारियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। याद रहे कि 2010 के बाद से जाने-माने कानून-उल्लंघनकर्ता अक्सर ऐसी जांच से साफ इनकार करते आ रहे हैं।
