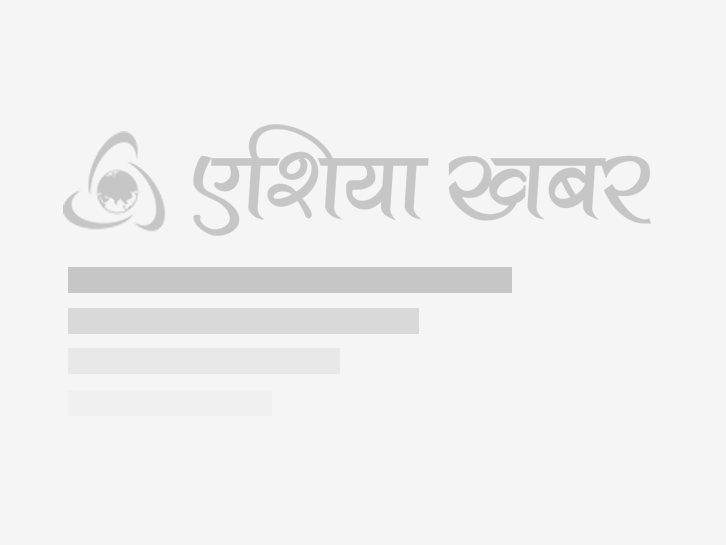
भारत के न्यायालय की ताजी तजबीज आई है कि ‘‘राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से देश-प्रेम का प्रकाशन नहीं माना जा सकता।’ ‘‘वन्दे मातरम’ को लेकर भी यहां-वहां यदा-कदा विवाद उठते रहते हैं। राष्ट्र भाषा को लेकर भी स्थिर मत नहीं बन पा रहा है। बहुलता और एकता का संतुलन बड़ी चुनौती बनी रहती है। भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर छिड़ने वाली बहस में अनेक दावे किए जाते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक प्रकृति, उसके इतिहास और सांप्रतिक प्रतिबद्धताओं से जुड़े होते हैं।यहां पर यह समझ लेना भी जरूरी होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद को सिर्फ आधुनिक पश्चिम के तर्ज पर उभरीं प्रक्रियाओं और संस्थाओं के खांचे में रख कर समझ पाना मुश्किल है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की बात भारतीय समाज में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में आई। अधिकांश नेता मान बैठे थे कि एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीय भावना को लाए बिना हम पिछड़े ही बने रहेंगे। उपनिवेश-विरोधी भारतीय राष्ट्रवाद के आतंरिक और बाह्य, दो पहलू दिखते हैं। बाह्य क्षेत्र में उपनिवेश की सत्ता के विरोध के साथ आंतरिक दुनिया में भी परिवर्तन घटित होते हैं, और संभवत: आंतरिक परिवर्तन राजनैतिक दुनिया के परिवर्तन का पूर्ववर्ती होता है। अत: राष्ट्रवादियों ने बाहरी दुनिया यानी आर्थिक क्षेत्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि को अपनाना यानी उनका अनुकरण करना हितकर माना। स्वीकार किया कि पश्चिम इन सब मामलों में हमसे श्रेष्ठ है। दूसरी ओर आंतरिक दुनिया में पश्चिम के प्रवेश को वर्जित मान कर अस्वीकार किया क्योंकि वे उनकी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के जरूरी अंग थे। अपनी एक विशिष्ट आध्यात्मिक संस्कृति को अक्षुण्ण बचाए रखना उनके लिए महत्त्वपूर्ण था। ‘‘राष्ट्र’ को आधुनिक विमर्श में एक कल्पित अवधारणा या संकल्पना मानते हैं, जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता और प्रभुता होती है परंतु ‘‘राज्य’ पर बाहरी साम्राज्य का ही दबदबा होता है। अत: जहां आधुनिक राष्ट्रीय संस्कृति की अवधारणा किसी पश्चिमी दखल को अस्वीकार करती है, वहीं राष्ट्रीयतावादी अभिजात वर्ग के नैतिक-बौद्धिक नेतृत्व को एक पश्चिमी ज्ञानोदय के सामजिक विचारों से कोई गुरेज न था। फलस्वरूप राज्य की व्यवस्था की संस्थाएं आधुनिक औपनिवेशिक राज्य की व्यवस्था के ही अनुकूल बनी रहीं। किसी विकल्प की खोज के बदले आधुनिक राज्य की पुरानी प्रचलित औपनिवेशिक अवधारणा को ज्यों का त्यों अंगीकार कर लिया गया। राष्ट्र एक संकल्पनात्मक समुदाय या समाज है, और राष्ट्र को राज्य होना है तो हमें समुदाय और राज्य, दोनों को एक साथ समझना होगा।पूंजी और समुदाय के रिश्ते भी गौरतलब हैं। पूंजी की अपनी अपेक्षाएं हैं, जो राष्ट्र राज्य या राष्ट्र की स्वीकृति से जुड़ी हैं। शायद राष्ट्र राज्य की अवधारण पूंजी के साथ ही चल सकती है। पूंजी सिर्फ राष्ट्र राज्य को ही स्वीकार करती है। सबको एक सा देखती है। पर हम देख रहे हैं कि समुदाय और उसकी विशिष्टता को खारिज नहीं किया जा सका और वह मौजूद है और पूरे दमखम के साथ। आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा से अप्रभावित राष्ट्रीय अस्मिता की बात महात्मा गांधी में मिलती है। वे राष्ट्रीय अस्मिता को सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थापित करते हैं। उनके हिसाब से शांति, उत्पादकता और सर्जनशीलता के साथ अनेक समुदाय एक साथ रह सकते हैं परंतु भारत में फलीभूत राष्ट्र राज्य की संकल्पना पश्चिमी विकास की धारा के ही अनुरूप है, जिसमें राज्य पूंजी के महाआख्यान से परिचालित होता है। राष्ट्र राज्य की संकल्पना में पूंजी और औपनिवेशिक सत्ता का सहज गठजोड़ निहित होता है। पं. नेहरू का राष्ट्रवाद, जो अंतत: राजनैतिक रूप से सफल लगता है, मूलत: एक उपनिवेश के विरोध में था। इस राष्ट्रवाद में स्थानीय देशभक्ति को भी स्थान था। बाद में आरक्षण जैसे हस्तक्षेप द्वारा भारतीय राजनीति का हुलिया ही बदल गया। आभिजात्य से अलग सामान्य और वंचित का प्रवेश हुआ। सार्वभौमिक आदर्श एक किस्म का नागरिक राष्ट्रवाद है, जो जाति, धर्म या संस्कृति से मुक्त हो कर व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार पर बल देता है। दूसरी ओर, सांस्कृतिक अस्मिता की विशिष्टता को स्वीकार करने की मांग है, जिसके आधार पर वंचित समूह के साथ, उनके पिछड़ेपन या ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय को ध्यान में रख कर भिन्न बर्ताव किया जाए। दोनों के बीच सतत तनाव बना हुआ है। वस्तुत: राष्ट्र का आधुनिक रूप सार्वभौम और विशिष्ट, दोनों ही तरह का है। याद रखना चाहिए की राष्ट्र चेतना अनेक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो मिल कर राष्ट्र का निर्माण करती हैं।
