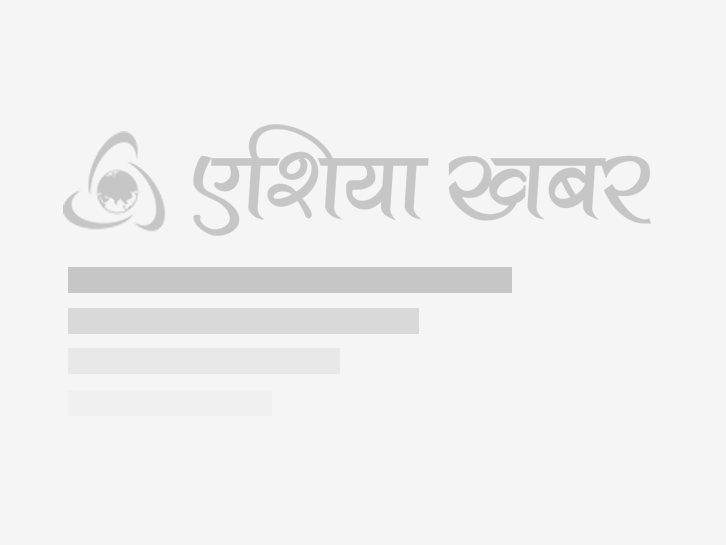
संयोग गुप्ता
दिल्ली में हुए खून-खराबे, जिसे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कहना बेहतर होगा, ने पूरे देश को हिला कर रख
दिया है. विभिन्न टिप्पणीकार और विश्लेषक यह पता लगाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस हिंसा के
अचानक भड़क उठने के पीछे क्या वजहें थीं. भारत में साम्प्रदायिक हिंसा के विश्लेषण में जिस एक कारक को
लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है वह है जाति. जाति को उन ग्रंथों की स्वीकृति और मान्यता प्राप्त है, जिन्हें
हम ‘हिन्दू धर्मग्रंथ’ कहते हैं. जातिप्रथा, हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का अविभाज्य अंग है, जिसकी चपेट में अन्य
धार्मिक समुदाय भी आ गए हैं. जहां हिन्दू राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व के संदर्भों में जाति के कारक का विस्तार से
विश्लेषण और अध्ययन हुआ है वहीं साम्प्रदायिक हिंसा में जाति की भूमिका के विश्लेषण को काफी हद तक
नजरअंदाज किया जाता रहा है.
सूरज येंगड़े ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के दिल्ली संस्करण में 8 मार्च 2020 को प्रकाशित अपने लेख में इस मुद्दे
पर कुछ समीचीन टिप्पणियां कीं हैं. वे लिखते हैं, “दिल्ली के दंगों को हिन्दुत्व व हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच
बैरभाव के संदर्भों में समझने के प्रयास हो रहे हैं. इसके पीछे इन दोनों में से कोई भी कारक नहीं है. दरअसल, इस
तरह की घटनाओं के लिए साम्प्रदायिक नहीं बल्कि जातिगत तनाव जिम्मेदार हैं.”
अपने लेख में येंगड़े ने गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता राजू सोलंकी के विश्लेषण का हवाला दिया है. राजू सोलंकी
लिखते हैं कि “सन् 2002 के गोधरा दंगों के सिलसिले में अहमदाबाद में कुल 2,945 लोगों को गिरफ्तार किया
गया था. इनमें से 1,577 हिन्दू थे और 1,368 मुसलमान. गिरफ्तार किए गए हिन्दुओं में से 797 ओबीसी थे,
747 दलित, 19 पटेल, 2 बनिया और 2 ब्राम्हण. इनमें से ऊँची जातियों के आरोपी तो विधायक बन गए और
अन्यों को जेल के सींखचों के पीछे डाल दिया गया. यह मात्र संयोग नहीं है कि भारत में सन 2015 में गिरफ्तार
किये गए व्यक्तियों में से 22 प्रतिशत दलित, 11 प्रतिशत आदिवासी, 20 प्रतिशत मुसलमान और 31 प्रतिशत
ओबीसी थे. जिन लोगों के विरूद्ध मुकदमे चले, उनमें से 55 प्रतिशत इन्हीं समुदायों से थे (एनसीआरबी,
2015).”
इन आंकड़ों की सत्यता को स्वीकार करते हुए भी यह कहा जा सकता है कि हिन्दुत्व की राजनीति के परवान चढ़ने
में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. परंतु जहां तक साम्प्रदायिक हिंसा का प्रश्न है, उसमें जहाँ धर्म की प्रमुख
भूमिका रहती है वहीं जाति दूसरा सबसे बड़ा कारक होती है. हिन्दू राष्ट्रवाद के झंडाबरदार आरएसएस के संबंध में
बिना किसी हिचक के कहा जा सकता है कि उसके उदय और उसकी ताकत में इजाफे का मुख्य कारण बढ़ती
जातिगत चेतना और जाति व वर्ण व्यवस्था से उपजे अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध था. आरएसएस के गठन
के पूर्व ही देश में हिन्दू महासभा अस्तित्व में आ चुकी थी. यह संगठन मुस्लिम लीग का विरोधी तो था परंतु एक
अर्थ में उसका समानांतर संगठन भी था. शुरूआत में इन दोनों संगठनों के सदस्यों में राजाओं और जमींदारों का
बोलबाला था परंतु बाद में समाज के श्रेष्ठि संपन्न वर्ग के कुछ लोग भी इनसे जुड़ गए.
आरएसएस का उदय मूलतः सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में आम लोगों और नीची जातियों के सदस्यों के प्रवेश
की प्रतिक्रिया था. नागपुर-विदर्भ क्षेत्र में ब्राम्हण-विरोधी आंदोलन और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग
आंदोलन से ब्राम्हणवादी इतने भयातुर हो गए कि उन्होंने राजाओं और जमींदारों के समर्थन और सहयोग से हिन्दू
राष्ट्र का झंडा उठा लिया. हिन्दुत्व की राजनीति के मूल में था प्राचीन भारत, जिसमें मनु संहिता का बोलबाला था,
का महिमामंडन. जोतिबा फुले और उनके बाद अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए अभियानों से दलितों का जो
सशक्तिकरण हो रहा था, ब्राम्हणवादी ताकतें उससे भयग्रस्त हो गईं थीं.
मूल मुद्दा तो यही था परंतु हिन्दुओं को एक करने के लिए यह आवश्यक था कि उनके किसी ‘बाहरी’ शत्रु का
अविष्कार किया जाए और इसके लिए मुसलमानों से बेहतर भला कौन हो सकता था? विशेषकर इसलिए क्योंकि
मुसलमानों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया था. इस तरह संघ का मूल एजेंडा दलितों को दलित बनाए
रखना था परंतु उस पर मुस्लिम-विरोध का मुल्लमा चढ़ा दिया गया. आरएसएस की शाखाओं और बौद्धिकों में
इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया गया. जहां मुसलमानों को प्रत्यक्ष शत्रु बताया गया वहीं
प्राचीन भारत का महिमामंडन कर लैंगिक और जातिगत पदक्रम को वैध ठहराने का प्रयास भी शुरू किया गया.
हिन्दुत्व के अभियान को जिस मुद्दे ने सबसे पहले हवा दी वह था एक मुस्लिम बादशाह द्वारा कथित तौर पर
भगवान राम की जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को ढ़हाया जाना. परंतु इस अभियान ने सन् 1990 में मंडल आयोग
की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद जोर पकड़ा. हिन्दुत्व की राजनीति, मुस्लिम-विरोध के साथ-साथ जातिगत
और लैंगिक पदक्रम को बनाए रखने का उपक्रम भी थी. हिन्दू राष्ट्रवाद के ताकतों का यही एजेंडा है. जहाँ तक
सांप्रदायिक दंगों का सवाल है, वे मूलतः मुसलमानों का कत्लेआम ही रहे हैं. आंकड़ों से यह साफ़ है कि सांप्रदायिक
हिंसा के पीड़ितों में से 80 प्रतिशत मुसलमान होते हैं. वे समाज के सभी आर्थिक वर्गों से होते हैं परन्तु इनमें
गरीबों की बहुतायत होती है.
दंगों को भड़काने में जाति की मुख्य भूमिका रहती है. हिंदुत्व के पैरोकार बड़े पैमाने पर दलितों के बीच सक्रिय रहे
हैं. भंवर मेघवंशी की हालिया पुस्तक, “आई वास ए स्वयंसेवक” बहुत बेहतर तरीके से यह बताती है कि किस प्रकार
दलितों को सांप्रदायिक हिंसा में शामिल किया जाता है. संघ ने सामाजिक समरसता मंच सहित कई ऐसे संगठनों
का जाल बिछाया है जो दलितों में ब्राह्मणवादी मूल्यों का प्रचार-प्रसार करते हैं और उन्हें हिन्दुत्ववादी राजनीति का
हिस्सा बना रहे हैं. दलितों का सांप्रदायिक दंगों में मोहरे की रूप में इस्तेमाल किया जाता है. वे सड़कों पर हिंसा
करते हैं जबकि नफरत फैलाने वाले, लोगों के दिमाग में जहर भरने वाले, अपने घरों और कार्यालयों में आराम से
बैठे रहते हैं.
गुजरात हिंसा के चेहरे अशोक मोची अब दलित-मुस्लिम एकता के समर्थक हैं. राजू सोलंकी द्वारा संकलित आंकड़े,
जिनका येंगड़े ने अपने लेख में हवाला दिया है, भारत में हिंसा की कहानी कहते हैं. जिन लोगों को भड़काया जाता
है और जिन्हें बाद में जेलों में ठूंस दिया जाता है, वे उन लोगों में से नहीं होते जो संघ को चंदा देते हैं और उसकी
विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करते हैं. सड़कों पर खून-खराबा करने वाले लोग होते हैं पददलित समुदायों के
गुमराह कर दिए गए युवक. सांप्रदायिक हिंसा में जाति की भूमिका को रेखांकित कर, येंगड़े ने एक महत्वपूर्ण काम
किया है. परन्तु उनके विश्लेषण में जो कमी है वह है धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने के अभियान
की भूमिका को कम करके आंकना क्योंकि यही हिंसा भड़काने का आधार होता है. शाखाओं के ज़रिये जिस तरह के
गलत तथ्य और बेबुनियाद धारणाएं लोगों के दिमाग में भरी जातीं हैं, वे अत्यंत प्रभावकारी सिद्ध होती हैं. यह
भंवर मेघवंशी के विवरण से स्पष्ट है, जिन्होनें बताया है कि उन्हें संघ के दुष्प्रचार की धुंध से बाहर निकल कर
जाति के यथार्थ को समझने में कितना वक्त लग गया.
